आध्यात्मिक प्रवचन
आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री
(वैदिक प्रवक्ता )
मैं कौन हूँ ? कहां से आया हूँ ? कहां जाऊंगा ? जन्म क्या है ? मृत्यु क्या है ? जीवन क्या है ? जीवन और जीवन की सफलता का आधार क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर जीवन रहते यदि नहीं मिला या उत्तर पाने का प्रयास नहीं किया तो समझो यह जीवन बेकार चला जाएगा।
इस चर्चा में हम इस प्रकार के प्रश्नों पर ही विचार विमर्श करेंगे – आशा है आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और मित्रों को भी पढ़ायेंगे।
आध्यात्मिक सिद्धान्तों को बहुत ही सुन्दर तरीके से समझाने में सफल कठोपनिषद् से चर्चा आरम्भ करते हैं – कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक ब्रह्मचारी यमाचार्य से प्रश्न करता है कि आत्मा की शरीर के मरने के बाद क्या गति होती है ? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर के मरने के बाद आत्मा भी मर जाती है ( आत्मा अनित्य है ) और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नही मरती है ( आत्मा नित्य है ) । हे आचार्य ! मैं यह जानना चाहता हूँ ?
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।
एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीय: ॥
नचिकेता कहता है –हे यमराज, मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई कहता है कि मृत्यु के उपरान्त उसके आत्मा का अस्तित्व रहता है और कोई कहता है कि नहीं रहता, कृपया मुझे इसे समझा दें। यह नचिकेता का अभीष्ट और श्रेष्ठ वर है।
गति जीवात्मा की कोई समझाये कहां से ये आये कहां लौट जाये
दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां
एक कुमार से ऐसे गूढ प्रश्न की आशा नहीं की जा सकती। अतएव यमदेव ने नचिकेता के सच्चा अधिकारी अथवा सुपात्र होने की परीक्षा ली। यमदेव ने देर तक उसे टालने का प्रयत्न किया, किन्तु यह सम्भव न हो सका। इससे संवाद में रोचकता आ गयी है।
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेषधर्म:।
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम् ॥
अध्यात्मविद्या दुर्विज्ञेय है। अग्निविद्या आदि कर्मकाण्ड के विषयों को समझना सरल है, किन्तु ब्रह्मविद्या का उपदेश करना और ग्रहण करना अत्यन्त कठिन है। यमदेव ने नचिकेता से कहा – यह विषय तो अत्यन्त गूढ है तथा सुगम नहीं है। अत: तुम कोई अन्य वर मांग लो और इस वर को मुझे ही छोड़ दो।
वास्तव में यमदेव केवल नचिकेता के औत्सुक्य को उद्दीप्त कर रहे हैं और उसकी पात्रता की परीक्षा ले रहे हैं, बल्कि उसके मन में ब्रह्मज्ञान की महिमा को प्रतिष्ठित भी कर रहे हैं।
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ।
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥
नचिकेता अपनी गहन उत्सुकता तथा निश्चय की दृढ़ता का परिचय देता है तथा यम द्वारा आग्रह न करने के परामर्श को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है – हे यमराज, आपका कथन ठीक है कि विद्वान भी आत्मतत्त्व के विषय में संशयग्रस्त हैं और निर्णय नहीं ले पाते, किन्तु आप मृत्यु के देवता हैं और आपके समान कोई अन्य उपदेष्टा यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि मृत्यु के उपरान्त् आत्मा का अस्तित्व रहता है अथवा नहीं। मेरे प्रश्न द्वारा याचित वरदान के तुल्य महत्त्वपूर्ण अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। यह एक विचित्र संयोग है कि आपके सदृश इस विषय का कोई अन्य ज्ञाता नहीं है और अध्यात्मविद्या के वर के समान अन्य कोई वर भी नहीं हो सकता।
शतायुष: पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान्।
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥
यमराज ने नचिकेता को एक कुमार के मन की अवस्था के अनुरुप धन-धान्य मांग लेने के लिए कहा। यमराज ने उसे दीर्घायुवाले बेटे-पोते, बहुत से गौ आदि पशु, गज, अश्व, भूमि के विशाल क्षेत्र, स्वयं की भी यथेच्छा आयु प्राप्त करने का प्रलोभन दिया और समझाया कि वह आत्मविद्या को सीखने के लिए उसे विवश न करे।
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च।
महाभूभौ नचिकेतस्त्वमेधिकामानान्त्वा कामभाजं करोमि॥
यमराज नचिकेता के मन को प्रलुब्ध करने के लिए अनेक कामोपभोगों की गणना करते हैं-अपार धन, जीवनयापन के साधन, विशाल भूमि पर शासन, अनन्त कामनाओं का भोगी। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि वह आत्मज्ञान के समान किसी भी अन्य वर को मांग ले, जिसे वह उपयुक्त समझता हो। वास्तव में यमाचार्य नचिकेता के मन में आत्मज्ञान के प्रति उसकी उत्सुकता बढा रहे हैं और उसकी पात्रता को परख भी रहे हैं।
ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दत: प्रार्थयस्व।
इमा रामा: सरथा: सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यै:।
आभिर्मत्प्रत्ताभि: परिचारयस्व नचिकेतो ! मरणं मानुप्राक्षीः ॥
यमाचार्य अनेक प्रकार से नचिकेता के अधिकारी (सुपात्र) होने की परीक्षा ले रहे हैं तथा मानवकल्पित सम्पूर्ण भोगों का प्रलोभन दिखा देते हैं। वे नचिकेता से कहते हैं कि वह स्वर्ग की अप्सराओं को, स्वर्गीय रथों और वाद्यों के सहित ले जाए जो मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए अलभ्य हैं तथा उनसे सेवा कराए, किन्तु आत्म ज्ञान विषयक प्रश्न न पूछे। किन्तु नचिकेता वैराग्य सम्पन्न और दृढनिश्चयी था। आत्मतत्त्व के सच्चे जिज्ञासु के लिए वैराग्यभाव तथा दृढनिश्चय होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह अपनी साधना में अडिग नहीं रह सकता।
श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज:।
अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥
नचिकेता ने आत्मज्ञान की अपेक्षा सांसारिक सुख भोगों को तुच्छ घोषित कर दिया (नाशवान = आज हैं तो कल नहीं रहेंगे), भौतिक सुखभोग इन्द्रियों की शक्ति को क्षीण कर देते हैं तथा उनसे शान्ति नहीं होती। इसके अतिरिक्त मनुष्य का जीवन अल्प और अनिश्चित है। अतएव जिस विवेकशील पुरुष के लिए सत्य साध्य है एवं प्राप्य है, उसके लिए ये भौतिक सुखभोग त्याज्य हैं। नचिकेता यमदेव से कह देता है कि उसे ये नश्वर भोग-पदार्थ प्रलुब्ध नहीं करते तथा इन्हें वह अपने पास ही रखें।
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा।
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय: स एव॥
नचिकेता ने एक परम सत्य का कथन किया है कि धन से मनुष्य की आत्यन्तिक तृप्ति नही हो सकती। उसने यमदेव को सम्मान देते हुए कहा – जब कि हमने आपके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, आपकी कृपा से धन तो हम पा ही लेंगे तथा आप जब तक शासन करते रहेंगे, हम भी तब तक जीवित रह सकेंगे। अत: धन और दीर्घायु की याचना करना व्यर्थ है।
कठोपनिषद् का पहला उपदेश नचिकेता के मुख से निस्सृत हुआ है।”न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य:” को कण्ठस्थ करके इसके सारतत्त्व को ग्रहण कर लेना चहिए। मनुष्य की आत्यन्तिक तृप्ति कभी धन-सम्पत्ति से नहीं हो सकती। मनुष्य धन से सुख-सुविधा के साधनों को प्राप्त कर सकता है, किन्तु हमेशा सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में धन बहुत कुछ है, किन्तु सब कुछ नही है।
दौलत के दीवानों उस दिन को पहचानो
जिस दिन भरी महफिल से खाली हाथ चलोगे क्या लेके साथ चलोगे
इच्छाओं की तप्ति भोग से नहीं होती, जैसे कि अग्नि की शान्ति घृत डालने से नहीं होती, बल्कि वह अधिक उद्दीप्त हो जाती है।
उपरोक्त प्रसंग के चिन्तन से एक बात स्पष्ट होती है कि आत्मज्ञान सर्वोत्तम है । नचिकेता के सम्मुख आत्मज्ञान के बदले में संसार का वैभव दिया जाता है लेकिन वह धीर पुरुष आत्मज्ञान को ही अपना लक्ष्य रखता है । और यही बात आज संसार के लोगों के सम्मुख रखी जाय तो आत्मज्ञान को चुनने वाले विरले ही मिलेंगे, संसार का वैभव पाने वाले ही अधिकतर होंगे। और इनमें भी सही रास्ते से धन कमाने वाले अब कम हो गये हैं , किसी भी तरह धन आये आज तो ऐसे लोगों की संख्या अधिक है।
आगे चर्चा बहुत बड़ी है क्रमशः आप पढेंगे कि वर्तमान समाज कैसा है और इसके दूरगामी परिमाण क्या होगें ? आत्मा कैसा है ? इसकी गति क्या होगी ? शरीर का विश्लेषण ? कर्म का आधार ? कर्म के साधन ? कर्म के प्रकार ? पाप पुण्य क्या है ? इनका फल क्या है ? क्या पाप के फल को किसी भी साधन या अनुष्ठान से बदला जा सकता है ? इत्यादि।
उपरोक्त चर्चा में हमने देखा कि आचार्य यम के द्वारा नचिकेता को आत्मज्ञान के बदले में संसार का वैभव मांगने को कहा तो नचिकेता संसार का वैभव यह कहकर ठुकरा देता है कि –
० संसार का वैभव स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं।
० भोग से रोग होते हैं शक्ति क्षीण होती है।
० आयु कितनी भी मांग लू एक दिन वह भी समाप्त हो जायेगी।
० धन से मनुष्य कभी सन्तुष्ट नहीं होता, पहले थोड़े धन की कामना करता है उसके मिलने पर कामना बढ़ती जाती है।
० हे आचार्य ! आपसे अच्छा मुझे समझाने वाला कोई नही मिलेगा इसीलिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त मैं कोई और भिन्न प्रश्न नही मांगता । कृपया मेरा कल्याण कीजिए।
उपरोक्त कथन पर महाराज मनु ने भी कहा –
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्ध्दते ॥
यह निश्चय है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता है वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये।
राजा भर्तृहरि वैराग्य शतक में इस विषय को कुछ इस तरह कहते है –
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।।
कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।।
भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें ही भोग लिया । तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए । काल (समय) कहीं नहीं गया बल्कि हम स्वयं चले गए । इस सभी के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गयी ( भोगों की इच्छा कमजोर नही हुई ) बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए ।।
कहावतें हैं –
० कि मनुष्य एक साथ ही भगवान् तथा धन को प्रेम नहीं कर सकता “Ye cannot serve God and a mammon.”
० ऊँट के लिए सुई में से गुजरना धनिक द्वारा परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने की अपेक्षा सरल है।” For it is easier for a camel to go through a needle’s eye than for a richman to enter into the kingdom of God.”
० आद्यात्मिक साधक के मार्ग में धन की तृष्णा एवं धन का अभिमान बाधक हैं। उसे सादगी और संतोष से जीवन-यापन करना चाहिए।
० धन की लिप्सा मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कर देती है।
० धन का प्रभाव धन के अभाव से अधिक दुःखदायक होता है।
० धन का लोभ मनुष्य को भटकाकर अशान्त बना देता है तथा धन की प्रचुरता मनुष्य को मदान्ध बना देती है।
कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय,
या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए।
यहाँ एक कनक से तात्पर्य भांग से है तथा दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण है
तात्पर्य है कि स्वर्ण अथवा धन के लोभ का मद ( नशा ) भांग के मद से भी सौ गुना अधिक बावरा बना देता है। भांग को खाने से नशा चढ़ता है जबकि स्वर्ण अर्थात् सोने को प्राप्त करने से लालच का नशा मानव को पागल कर देता है ।।
धन की प्रचुरता प्रायः मनुष्य को विलासिता, दुर्व्यसन, अपराध, हिंसा और अशान्ति की ओर ले जाती है।
वास्तव में धन में दोष नहीं है, धन की लिप्सा एवं आसक्ति में दोष होता है। मनुष्य धन के सदुपयोग से दीन दुःखी जन की सेवा आदि लोक-कल्याण के कार्य कर सकता है। अतः हमें त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए।
यजुर्वेद में लिखा है –
ईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥
अर्थात् हे मनुष्य ! तू जो प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यन्त सब जड़ चेतन जगत है वह ईश्वर ( सकल ऐश्वर्य से सम्पन्न, सर्वशक्तिमान परमात्मा) के द्वारा आच्छादित अर्थात् सब ओर से अभिव्याप्त किया हुआ है। इसीलिए त्याग पूर्वक उपभोग कर। और यह धन किसका है अर्थात् किसी का नही यह तो उपभोग के लिए परमेश्वर से प्राप्त होता है; अतः किसी के भी धन वा वस्तुमात्र की अभिलाषा मत कर अपितु पुरुषार्थ कर।
उपरोक्त विषय पर महात्मा चाणक्य का कथन है –
सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने |
त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः ||
मानव का यह कर्तव्य है कि इन तीन स्थितियों में वह सदैव सन्तुष्ट रहे – (१) अपनी पत्नी के साहचर्य से (२) पवित्र कर्म से प्राप्त भोजन से, तथा (३) पुरुषार्थ से प्राप्त धन से | परन्तु इन तीन स्थितियों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिये – (१) विद्याध्ययन (२ ) मन्त्र जाप से ईश्वर की आराधना तथा (३) समाज के कल्याण हेतु दान करना |
परिश्रम और सच्चाई से धन अर्जित करना, जो भी प्राप्त हो जाय उसमें सन्तोष करना तथा उसका सदुपयोग करना विवेक सम्मत है।
यह एक तथ्य है कि मनुष्य सब कुछ यहीं एकत्रित करता है और सब कुछ यहीं छोड़कर सहसा चला जाता हैं। यदि सब कुछ छूटना है तो हम उसे स्वयं ही छोड़ दें अर्थात् उसके ममत्व, स्वामित्व और आसक्ति के भाव को छोड़कर भारमुक्त हो जाएँ। सब धन परमात्मा का ही है। अतः ‘इदं न मम’ (यह मेरा नहीं है। ) की भावना को शिरोधार्य करके धन का उपभोग एवं सदुपयोग करना सब प्रकार से श्रेष्ठ है।
निश्चय ही आत्मज्ञान की अपेक्षा धन अत्यन्त तुच्छ है। बृहदारण्यक उपनिषद् में जब मैत्रेयी के सम्मुख याज्ञवल्क्य ऋषि ने भौतिक सुख-सामग्री देने का प्रस्ताव रखा तो मैत्रेयी ने पूछा –
यन्नु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेनाहं अमृता स्यामिति।
अगर सारी पृथिवी धन-धान्य से भरपूर होकर मुझे प्राप्त हो जाय तो क्या मुझे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी ?
याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया –
यथैवोपकरणावतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन।
जैसे साधन-सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन होता है, वैसा तेरा जीवन हो जायेगा, परन्तु अमर-आनन्द तुझे प्राप्त नहीं होगा।
यह सुनकर मैत्रेयी ने जो उत्तर दिया, वह आज के भौतिकवादी युग को चुनौती है। उसने कहा,
येनाहं नामृता स्याम् किमहं तेन कुर्याम्।
जिस मार्ग पर चलने से मुझे अमरत्व की प्राप्ति न होगी, उस पर चल कर मैं क्या करूँगी ?”
इसलिए आज इस बात की अत्यधिक आवश्यकता होने लगी है कि अध्यात्म के मार्ग पर अनुसरण किया जाये और जीवन सुन्दर और सुखमय बनाया जाए। जीवन का उद्देश्य तो अमृतस्वरूप आत्मा को जानकर अमृतत्व प्राप्त करना है। उपनिषदों में अनेक स्थलों पर अमृतत्व की चर्चा है। जीवनकाल में आत्मतत्त्व को जानकर अमृतत्व प्राप्त करना ही उत्तम धन है। यही मानव की सर्वोच्च उपलब्धि भी है।
अभी तक कुछ विद्वानों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें कौन सा पथ चयन करना हैं। आगे हम समझेंगे कि वैदिक काल के लोग किस पथ का अनुसरण करते थे और आज के व्यक्ति ने कौन सा पथ चयन किया है।
अभी तक हमने समझा कि दो मार्ग हैं।
– एक संसार के वैभव पाने का भौतिक मार्ग और दूसरा परमेश्वर के आनन्द को पाने का आध्यात्मिक मार्ग इस विषय में उपनिषद में कहा है कि जीवन के दो पथ होते है – श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग इन्हें ही प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग भी कहा जाता है।
अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन् मर्त्यः व्कधःस्थः प्रजानन्।
अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदानदीर्घे जीविते को रमेत ॥
नचिकेता कुमारावस्था में ही बुद्धि की परिपक्वता एवं जिज्ञासा की गहनता का परिचय देता है। वह यमदेव से कहता है कि जीर्ण हो जानेवाला तथा मृत्यु को प्राप्त होनेवाला, मृत्युलोक में रहनेवाला, कौन मनुष्य जीर्ण न होनेवाले अमृतस्वरूप महात्माओं का संग पाकर भी भौतिक भोगों का चिन्तन करते हुए दीर्घकाल तक जीवित रहने में रुचि लेगा? यमराज जैसे महात्मा का सान्निध्य पाकर भी भोगों का चिन्तन करने की मूर्खता कौन विवेकशील मनुष्य करेगा? मृत्युलोक में रहनेवाले मरणधर्मा मनुष्य के लिए यमराज के सान्निध्य में आकर आत्मज्ञान की प्राप्ति से बढ़कर अन्य कौन-सा सौभाग्य हो सकता है? नचिकेता ने आत्मज्ञान के लिए आवश्यक वैराग्यभाव को प्रदर्शित करके स्वयं को उपदेश का सच्चा अधिकारी सिद्ध कर दिया। यह प्रसिद्ध ही है कि विषय-वासना और भौतिक वस्तुओं की तृष्णा से ग्रसित मनुष्य आत्मज्ञान की साधना नहीं कर सकता। नचिकेता सत्य का गम्भीर अनुसन्धाता है तथा संसार के सुखभोगों को तुच्छ समझकर उनका परित्याग करने पर दृढ़ है। वह मात्र दीर्घजीवी नहीं, दिव्यजीवी होना चाहता है।
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्।
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥
नचिकेता अपने निश्चय पर दृढ़ है तथा कोई प्रलोभन उसे विचलित नहीं कर सकता। यमराज जैसे उपदेष्टा के सान्निध्य का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करके वह उसे खोना नहीं चाहता। यमराज ने जितने भी प्रलोभन प्रस्तुत किए, नचिकेता ने उन सबको तुच्छ एवं हेय कह दिया। आत्मतत्त्व के ज्ञान से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। नचिकेता का तृतीय वर गूढ है और गंभीर विवेचना की अपेक्षा करता है।
भौतिक सुखों के नाना प्रलोभनों से उत्तीर्ण नचिकेता को आत्मज्ञान का योग्य अधिकारी समझकर यमाचार्य विद्या और अविद्या के भेद का कथन करते हैं –
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः ।
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ।।
हे नचिकेता ! अतिशय प्रशंसित कल्याण का मार्ग अर्थात् मोक्ष प्राप्ति का साधन रूप कर्म लौकिक अभ्युदय की अपेक्षा विलक्षण और दूसरा है और अतिशय प्रिय लगने वाला लौकिक स्त्रीधनैश्वर्यादि अभ्युदय का मार्ग मोक्ष मार्ग से भिन्न ही है वे श्रेय और प्रेय दोनों भिन्न-भिन्न प्रायोजन वाले मनुष्य को कर्म-फल रुप रस्सियों से बांधते हैं। उन दोनों में से कल्याणकारी मोक्ष-मार्ग को ग्रहण करने वाले का अच्छा फल होता है और जो अत्यन्त प्रिय वस्तुओं को स्वीकार करता है वह मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष रूप प्रायोजन से भ्रष्ट हो जाता है।
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ।।
मनुष्य को श्रेय = कल्याण मार्ग और प्रेय = अतिशय प्रिय धनैश्वर्यादि का मार्ग ये दोनों प्राप्त होते हैं अर्थात् संसार में दोनों मार्ग देखने में आते हैं परन्तु विवेकी विद्वान् पुरुष उन दोनों मार्गों को शास्त्रों के अनुशीलन से शुद्ध हुई बुद्धि से निश्चय कर प्रेयमार्ग से कल्याण मार्ग को निश्चय से सर्वथा स्वीकार करता है तथा मन्द बुद्धि पुरुष अथवा अविवेकी पुरुष भौतिक सुखों के साधनों के योग = उपार्जन और क्षेम = उनके रक्षण के कारण अत्यन्त प्रिय लगने वाले भोगों के मार्ग को ही स्वीकार करता है।
प्राचीन भारत का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि अधिकतर लोग श्रेय मार्ग पर चलने वाले ही होते थे।
प्रत्येक व्यक्ति साधना का जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरण के रुप में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी महाराज का जीवन देख सकते हैं जिन्होंने सत्य, न्याय और कर्तव्य पालन करते हुए अपने जीवन को कल्याण मार्ग पर ही रखा चक्रवर्ती राज्य को भी तुच्छ समझा , साथ की हम भ्राता भरत जी का जीवन भी इसी मार्ग का अनुगामी पाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज तो आध्यात्मिक मार्ग दर्शाते हैं धन-ऐश्वर्य तथा राज्यादि को सामान्य समझते हैं ( देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान योगी के बारे में अज्ञानता के कारण गलत मान्यतायें भी प्रचारित की जाती हैं)
गुरुवर स्वामी विरजानन्द सरस्वती जी महाराज विश्व कल्याण की भावना से साधना का जीवन जीते है।
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज के जीवन से कितने की लोगों को कल्याण मार्ग मिलता है , ऋषिवर संसार के वैभव को अनेक बार ठुकरा देते हैं विरुद्ध वातावरण होते हुए भी उन्हें साधना और विश्व कल्याण के मार्ग पर चलने से कोई भी बाधा नहीं रोक पायी।
कल्याण मार्ग का पथिक हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती जी महाराज तथा अनेक विद्वान और क्रान्तिकारियों का जीवन हम सभी के लिए प्रेरक बन गया है।
आज हमें इनके आदर्शों पर चल कर अपने जीवनों को कल्याण मार्ग पर ले जाना चाहिए। लेकिन आज तो अधिकतर लोग प्रेय मार्ग पर चलने वाले हैं इसीलिए केवल संसार के वैभव को ही पाने का उद्यम करते है।
इनमें से भी ऐसे लोग कम हैं जो पुरुषार्थ से धन अर्जित करते है और अधिक लोग ऐसे हैं जो किसी भी अनैतिक साधन से धन इकट्ठा करते हैं।
० धन के लिए पशु-पक्षियों को काटकर बिक्री कर देते, आजकल तो मनुष्यों का भी मांस बिक रहा है।
० धन के लिए मनुष्यों को मारकर लूट की जाती है तथा धन वैभव पाने के लिए सम्बन्धियों के साथ साथ माता-पिता और रक्त सम्बन्धियों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है ।
० उपयोगी सामान और पशुओं की चोरी तो बहुत समय से होती हैं अब तो फिरोती के लिए मनुष्यों का अपहरण कर लिया जाता है, तथा एक अनैतिक कार्य ने तो हमें बहुत ही दुःखी किया है वह यह है कि छोटे बच्चों का अपहरण करके फिरोती नहीं मागीं जाती बल्कि उनके आन्तरिक अंगों को निकाल कर बेच दिया जाता है यह कितना जघन्य अपराध है लेकिन धन पाने के लिए यह सब भी हो रहा है।
० रिश्वतखोरी का हाल तो आप सब जानते हैं अब तो इसकी भी नयी नयी तकनीकें विकसित हो गई हैं जिनसे दूसरे का धन अधिक से अधिक ठगा जासके।
० कमीशन का दौर तो ऐसा चला कि जिसमें सारा समाज बहुत अच्छे से जकड़ गया है। आपातकाल में मुझे कानपुर से दिल्ली तक बस से यात्रा करनी थी बस तक पहुंचने के लिए ऑटोरिक्शा लिया उसे मार्गव्यय भी दिया लेकिन बस वाले से भी ऑटोरिक्शा वाले ने एक सवारी का कमीशन भी ले लिया । जब मैंने बस में बैठने से पहले किराया पूछा। मुझे किराया अधिक लगा तो मैं बस में नही बैठा तो इस पर बस वाला बहुत नाराज हो गया । जब मैंने नाराजगी का कारण पूछा तो बताया कि आपका यात्रा का कमीशन रिक्शा वाले को दिया है उसका क्या । तब हमने उससे कहा कि यह आपका विषय है।
मित्रो ! हो सकता है कि ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा । हां वह अलग बात है कि यात्रा में नही हुआ हो किसी अन्य स्थान पर हुआ हो क्योंकि इस कमीशन की माया से कोई भी विभाग अछूता नही रहा है । इसका जाल चिकित्सा, शिक्षा, न्याय, यात्रा, सभी प्रकार के क्रिय-विक्रय आदि में सर्वव्यापक होगया है।
० मिलावट इस तरह हुई है कि अब बाजार में कोई भी सामान विश्वास के साथ नहीं मिलता है। मिलावटी सामान शुद्ध से भी शुद्ध लगता है । आश्चर्य तो तब होता है कि जब बिना पशुओं के दूध तैयार हो जाता है और बिना दूध के मावा तैयार हो जाता है। एक समय था जब बाजार में घी वाली दुकान पर जाकर कहा जाता था की घी चाहिए तो दुकानदार कहता था कि कितना दे दूं, लेकिन आज यदि कहोगे कि घी चाहिए तो दुकानदार कहेगा कि कौन सा और कितना चाहिए अर्थात् एक समय था जब घी के नाम पर एक देशी घी ही होता था और वह भी शुद्ध ही होता था लेकिन आज मिलावटी घी है और अनेक प्रकार का है। पिसे हुये मसालों में अखाद्य रंग मिला हुया है जो कि हानिकारक कैमिकल युक्त है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिले हैं। धनिये में भूसा और बुरादा तथा गोबर तक मिला हुआ है। लाल मिर्च में गेरू और रंग मिला हुआ है। दूध में यूरिया, साबुन व एसिड, नमक में चॉक पाउडर, हल्दी में डाई वाला कलर, देसी घी में वनस्पति तेल, स्टार्च आदि की मिलावट होरही है।
अनेक अनैतिक तरीकों से धन कमाने वाला स्वयं को बहुत चतुर समझता है लेकिन यथार्थ इससे बिल्कुल अलग है = एक तो यह कि सुख का सच्चा साधन विद्या और सत्य व्यवहार ही है और दूसरा किये हुए कर्म का भुगतान अवश्य ही करना होता है इस सन्दर्भ में हम आगे विस्तार से लिखेंगे। अभी तो हम नचिकेता के प्रश्न आत्मा की गति पर विचार करेंगे।
अब हम नचिकेता के प्रश्न (शरीर के मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है?) पर यमाचार्य के उत्तर का विश्लेषण करेंगे। यमाचार्य नचिकेता को आत्मज्ञान के सन्दर्भ में उपदेश करते है –
न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥
यमाचार्य नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि (न हन्यते हन्यमाने शरीरे ) शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरता है । वैसे तो संक्षेप में यह उत्तर हो गया लेकिन इतने उत्तर से काम नहीं चलेगा इसीलिए आगे कहते हैं कि (न जायते न म्रियते ) आत्मा न जन्म लेता है और न ही मरता है । ऐसा कहने पर पुनः नया प्रश्न उपस्थित होता है कि संसार में तो जन्म और मृत्यु देखने में आता है और यमाचार्य कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म – मृत्यु नही होता है। इस प्रसंग को इस प्रकार समझेंगे कि संसार में ऐसी बहुत सी घटनायें होती है जो होती तो कुछ हैं और कही कुछ जाती हैं । जैसे रेलगाड़ी में यात्रा करने वाला एक दूसरे से कहता है कि देखना भाई कौन सा स्टेशन आगया और उत्तर देने वाला भी कह देता है कि अमुख स्टेशन आगया जबकि प्रश्न भी गलत है और उत्तर भी गलत है क्योंकि स्टेशन नही आता है यात्री स्टेशन पहुंचते हैं इसीलिए यह कहना चाहिए कि हम कौन से स्टेशन पहुंच गये या गाड़ी कौन से स्टेशन पहुंच गयी और उत्तर देने वाला कहना चाहिए कि हम या गाड़ी अमुख स्टेशन पहुंच गये।
एक और उदाहरण लेते हैं – हम यदि यह प्रश्न करें कि क्या सूर्य – उदय अस्त होता है तो कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य उदय – अस्त होता है और कुछ लोग कहेंगे कि सूर्य उदय अस्त नहीं होता है और कुछ तो कहेंगे कि उदय अस्त होते दिखाई नहीं देता है क्या। लेकिन यथार्थ तो यही है सूर्य का उदय और अस्त कभी नहीं होता है लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य का उदय अस्त दिखाई देता है वैसे ही जैसे गाड़ी में चलने वाले व्यक्ति को वृक्ष पीछे की ओर दौड़ते दिखते हैं। इसी प्रकार आत्मा का जन्म मृत्यु नही होता आत्मा शरीर में आजाती है तो जन्म सा दिखाई देता है और आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो मृत्यु सी दिखाई देती है। अर्थात् आत्मा और शरीर के संयोग का जन्म है तथा आत्मा और शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है। अभी हम आत्मा के विषय में समझ रहे हैं आगे हम शरीर के बारे में विस्तार से जानेंगे।
आत्मा की अमरता के विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं –
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।
आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सूखा नहीं सकता । अर्थात् आत्मा को किसी भी साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा एक अविनाशी और अनादि तत्व है।
आत्मा के बारे में एक बात अधिक जानने योग्य है ( जो ऐसा मानते हैं कि आत्मा तो परमात्मा में से बनती है, उनको यह बात अधिक ध्यान देकर समझनी चाहिए) यमाचार्य कहते हैं आत्मा किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है अर्थात् इसका कोई उपादान कारण नही है। आत्मा किसी में से बना नही है और ना ही इसमें से कुछ बनेगा।
इस विषय पर योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की बात बहुत प्रासंगिक लगती है वे कहते हैं कि –
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात् हम पहले भी हमेशा थे और आगे भी हमेशा रहेंगे।
ऋग्वेद में अविनाशी व अनादि तत्वों के बिषय इस प्रकार कहा है –
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते |
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ||
( द्वा ) जो ब्रह्म और जीव दोनों ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश ( सयुजा ) व्याप्य – व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त , सनातन अनादि हैं ; और ( समानम् ) वैसा ही ( वृक्षम् ) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न – भिन्न हो जाता है , वह तीसरा अनादि पदार्थ ; इन तीनों के गुण , कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं । ( तयोरन्यः ) इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है , वह इस वृक्षरूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को ( स्वाद्वत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है , और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को ( अनश्नन् ) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्वर , ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न-स्वरूप तीनों अनादि हैं ।
यमाचार्य आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं – (न) नहीं (जायते)उत्पन्न होता है (न) नहीं (म्रियते) मरता है (वा) या (विपश्चित) चेतनरूप, मेधावी (अयम्) यह (कुतश्चित्) कहीं से किसी उपादान कारण से (न, बभूव) उत्पन्न नहीं हुआ (कश्चित्) कोई (इससे भी उत्पन्न नहीं हुआ) (अजः) जन्म नहीं लेता (नित्यः) नित्य (शाश्वत:) अनादि हमेशा रहनेवाला (अयम्) यह (पुराणः) सनातन है (शरीरे) शरीर के (हन्यमाने) नाश होने पर (न, हन्यते)नष्ट नहीं होता ॥
अभी तक हमने समझा कि आत्मा (जीव) एक अविनाशी और अनादि तत्व है इसका जन्म-मृत्यु नही होता है । शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म कहलाता है और शरीर और आत्मा के साथ साथ चलने का नाम जीवन है तथा शरीर और आत्मा के वियोग का नाम मृत्यु है । शरीर छोड़ने पर आत्मा की क्या गति होती है इस पर आगे चर्चा करेंगे । इस चर्चा में अभी हम शरीर को समझेंगे।
उपरोक्त चर्चा में हमने समझा कि आत्मा (जीव) एक अविनाशी और अनादि तत्व है इसका जन्म-मृत्यु नहीं होता है । आत्मा परमात्मा से पृथक सत्ता है। शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म कहलाता है और शरीर और आत्मा के साथ साथ चलने का नाम जीवन है तथा शरीर और आत्मा के वियोग का नाम मृत्यु है । शरीर छोड़ने पर आत्मा की क्या गति होती है इस पर आगे चर्चा करेंगे । इस चर्चा में अभी हम शरीर को समझेंगे।
शरीर के बारे में सामान्यतः एक बात प्रचलित है कि शरीर तो पांच तत्वों – अग्नि, जल , वायु, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है।
शरीर को ठीक से समझने के लिए आइये कुछ चिन्तन करते हैं। शरीर विज्ञान के ज्ञाता प्राचीन आयुर्वेदाचार्य महर्षि चरक ने अपने शिष्यों को शरीर के विषय में समझाने के लिए एक इतिहास में हुई शरीर विज्ञान की चर्चा सुनाई । एक बार हिमालय के पास हुई परिषद में अनेक महर्षि सम्मिलित हुये। परिषद का विषय – “शरीर और शरीर के रोगों का कारण क्या है?” था। तथा परिषद के अध्यक्ष भगवान आत्रेय बनाये गये। सर्व प्रथम काशीपति वामक ने उपरोक्त प्रश्न को सभा में रखा जिसपर विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार दिये। जिसमें ऋषि कांकायन ने कहा कि शरीर और शरीर के रोगों का कारण परमात्मा है। परमात्मा ही शरीर देता है तथा वही स्वास्थ्य और रोग देता है। इस पर महर्षि भरद्वाज ने इसका कारण स्वाभाविक होना बताया। भद्रकाप्य ने कर्म को, ऋषि हिरण्याक्ष ने धातुओं को तथा ऋषि कौशिक ने माता-पिता को शरीर और शरीर के रोगों का कारण कहा। सभी के विचारों को सुनने के बाद सभाध्यक्ष महर्षि भगवान आत्रेय ने काशिपति के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केवल आहार ही शरीर का कारण होता है और अहितकर आहार का उपयोग ही रोग और रोगों की वृद्धि का कारण होता है।
यह बात अधिक ध्यान देने योग्य है कि शरीर आहार (भोजन) से बना है । इस बात पर पुनः शिष्यों ने आचार्य चरक से पूछा कि शरीर आहार से कैसे बना है तो उत्तर में आचार्य चरक कहते हैं कि शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है और बहुत ही छोटा होता है (लगभग सरसों के दाने के समान छोटा) यह छोटा सा शरीर माता और पिता के रज और शुक्र से मिलकर बनता है तथा रज और शुक्र आहार (भोजन) से बनता है।
शरीर का विज्ञान समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि आहार( जो भी भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है ) से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि (हड्डी) बनती है, अस्थि से मज्जा तथा मज्जा से रज और वीर्य बनता है जिससे सन्तान का शरीर बनता है।
माता के गर्भ में सन्तान के शरीर का विकास माता के किये भोजन से होता है। परमेश्वर की व्यवस्था में गर्भस्थ शिशु की नाभि माता की नाभि से जुड़ जाती है और उसी से उसका पोषण होता है। माता के किये भोजन का एक हिस्सा रस बनकर गर्भस्थ शिशु का निर्माण करता है।
जन्म के बाद कुछ समय तक शिशु का पोषण माता का दुग्ध पान करके होता है और वह दुग्ध माता के आहार से बनता है। हमारा शरीर भोजन से ही बनता है और भोजन से ही चलता है।
अभी तक हमने समझा कि शरीर का निर्माण भोजन से हुआ है और अब समझेंगे कि भोजन का निर्माण पांच तत्वों से ही होता है। भोजन में ठोस पदार्थ पृथ्वी का हिस्सा है, तरल पदार्थ जल का है, उर्जा अग्नि का, गैसीय पदार्थ वायु का व खाली स्थान आकाश का हिस्सा है। यदि हम दर्शन की बात करें तो कहा जा सकता है कि भोजन में जो गन्ध है वह पृथ्वी से आती है क्योंकि “गन्धवती पृथ्वी ” अर्थात् पृथ्वी का गुण है गन्ध, और रस जल से आया है, रंग अग्नि का गुण है । अर्थात् शरीर भोजन से बना है और भोजन प्राकृतिक तत्वों से बना है।
लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पांचों तत्व तो मिट्टी और लकड़ी आदि में भी हैं तो क्या हम मिट्टी या लकड़ी आदि खा सकते है शरीर बनाने या चलाने के लिए? तो इसका उत्तर होगा कि नहीं। जबकि कुछ जीव परमेश्वर ने ऐसे भी बनाये है जो मिट्टी या लकड़ी आदि खाकर जीवन चलाते हैं। इस विषय में यहां तो बस इतना ही कहेंगे कि मनुष्य को बहुत अच्छे से यह जानकर कि क्या खाना चाहिए और क्या नही खाना चाहिए हितकारी भोजन ही करना चाहिए । जिससे हमें हानि हो वह पादार्थ सेवन नहीं करना चाहिए (इस विषय पर विस्तार से कभी चर्चा करेंगे)।
अभी हमने आयुर्वेद के आधार पर यह जाना कि हमारा शरीर भोजन से बना है और भोजन पांच तत्वों – अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है।
यमाचार्य शरीर के विषय में नचिकेता को समझाते हैं –
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।।
इस जीवात्मा को तुम रथी, रथ का स्वामी, समझो, शरीर को उसका रथ, बुद्धि को सारथी, रथ हांकने वाला, और मन को लगाम समझो ।
इंद्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।।
मनीषियों, विवेकी पुरुषों, ने इंद्रियों को इस शरीर-रथ को खींचने वाले घोड़े कहा है, जिनके लिए इंद्रिय-विषय विचरण के मार्ग हैं, इन्द्रियों तथा मन से युक्त इस आत्मा को उन्होंने भोग करने वाला बताया है ।
प्राचीन भारतीय विचारकों का चिंतन प्रमुखतया आध्यात्मिक प्रकृति का रहा है । ऐहिक सुखों के आकर्षण का ज्ञान उन्हें भी रहा ही होगा । किंतु उनके प्रयास रहे थे कि वे उस आकर्षण पर विजय पायें । उनकी जीवन-पद्धति आधुनिक काल की पद्धति के विपरीत रही । स्वाभाविक भौतिक आकर्षण से लोग स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करें ऐसा वे सोचते रहे होंगे और उपनिषद् आदि ग्रंथ उनकी इसी सोच को प्रदर्शित करते हैं ।
उनके दर्शन के अनुसार अमरणशील आत्मा शरीर के द्वारा इस भौतिक संसार से जुड़ी रहती है और यहां के सुख-दुःखों का अनुभव मन के द्वारा करती हैं । मन का सम्बन्ध बाह्य जगत् से इन्द्रियों के माध्यम से होता है । दर्शन शास्त्र में दस इन्द्रियों की व्याख्या की जाती हैः पाँच ज्ञानेन्द्रियां (आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा) और पाँच कर्मेन्द्रियां (हाथ, पांव, मुख, मलद्वार तथा उपस्थ यानी जननेद्रिय, पुरुषों में लिंग एवं स्त्रियों में योनि)। उक्त श्लोकों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या नहीं का निर्धारण बुद्धि करती है और मन तदनुसार इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है । इन श्लोकों का सार यह है: भौतिक भोग्य विषयों रूपी मार्गों में विचरण करने वाले इंद्रिय रूपी घोड़ों पर मन रूपी लगाम के द्वारा बुद्धि रूपी सारथी नियंत्रण रखता है ।
यमाचार्य ने शरीर को रथ कहा है इससे अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं जैसे –
आत्मा को रथ प्राप्त कैसे होता है?
रथ बनता कैसे है?
रथ चलता कैसे है?
रथ से जाना कहां हैं?
इन प्रश्नों के उत्तर में अभी तो बस इतना ही कहना होगा (विस्तार से आगे चर्चा होगी)-
आत्मा को रथ (शरीर) कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है।
रथ (शरीर) प्राकृतिक पदार्थों से बनता है।
रथ (शरीर) को आत्मा चलाती है। आत्मा बुद्धि पूर्वक मन को इन्द्रिय के साथ जोड़कर कर्म करती है। शरीर साधन है।
रथ (शरीर) रूपी साधन से आत्मा को परमेश्वर के आनन्द को प्राप्त करना है ।
शरीर के सन्दर्भ में उपरोक्त विषयों पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
उपरोक्त चर्चा में हमने समझा कि आत्मा को कर्म करने के लिए साधन के रूप में शरीर प्राप्त होता है। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, दश इन्द्रियाँ घोड़े हैं।
यहां अभी हम केवल इस प्रसंग को विस्तार देते है कि शरीर प्रकृति से बनता है और इसको समझने के लिए रथ के स्थान पर (आज के समय में) गाड़ी को लेते हैं ( रथ = गाड़ी ) ।
हम गाड़ी खरीद कर लाते हैं, चलाते रहते हैं, खराव हो जाने पर मैकेनिक से ठीक करा लेते हैं और फिर चलाते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब मैकेनिक कहता है कि अब आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी बहुत पुरानी हो गयी है या ठीक होने लाइक नही है अब इसे बेचकर नयी ले लीजिए। पुरानी गाड़ी कबाडे़ वाले को देदेते हैं और नयी गाड़ी खरीद लेते हैं । अभी हम नयी गाड़ी के बारे में बात नही करेंगे , अभी देखते हैं पुरानी गाड़ी का क्या होगा। कबाड़े वाला गाड़ी को खोलकर उसके सभी हिस्सों को धातुओं के अनुसार अलग अलग इकट्ठा करता है। लोहा एक तरफ, प्लास्टिक एक तरफ, एल्मोनियम आदि धातुओं को अलग अलग रखता है। फिर कोई तो उन धातुओं को भट्टियों में डालकर शुद्ध करता है और उस उस शुद्ध धातुओं से नया सामन या गाड़ियों के पुर्जे बनाये जाते हैं । अर्थात् गाड़ी की सभी धातुएँ पुनर्चक्रण में काम आती हैं।
अब हम शरीर को देखेंगे कि यह शरीर भी गाड़ी की तरह से है क्या? तो हम पायेंगे कि बिल्कुल गाड़ी की तरह ही है।
यह शरीर भी खरीदा जाता है इसे खरीदने के लिए कर्म रूपी धन देना पड़ता है। अर्थात् हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें शरीर प्राप्त होता है ।(इसकी चर्चा विस्तार से आगे लिखेंगे।) इस शरीर को चलाते रहते हैं तथा खराब होने पर इसे भी गाड़ी की तरह मैकेनिक (डाक्टर) से ठीक कराते रहते हैं । एक दिन इसका मैकेनिक – डाक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, और कहता है कि इसे ले जाओ अब यह ठीक नही होगा/होंगे ( वो कोई भी हो सकते हैं हमारे सम्बन्धी) तब हम उन्हें अपने घर ले आते हैं ।
यहां एक बात बताना बहुत ही आवश्यक है = वृद्धावस्था में उपरोक्त स्थिति बनने पर – जिनकी सन्तान संस्कारित होती है तो अपने वृद्धों की सेवा करती है तथा जिनकी सन्तान संस्कारित नही होती है उनको इस स्थिति से गुजरने पर बहुत कष्ट होता है। इसीलिए वक्त रहते सन्तान को संस्कारित अवश्य करना चाहिए। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ हम दो उदाहरण रखते हैं –
१. एक वृद्ध व्यक्ति ऐसी स्थिति में आगये जिनके लिए डाक्टर ने कह दिया कि अब हम इनका उपचार नही कर सकते, इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए ये ऐसी स्थिति में हैं कि कुछ दिन के ही हैं। उनके पुत्र उनको घर पर ले गये और सेवा तो पहले से ही कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपने पिता की सेवा में कुछ ऐसा किया कि उदाहरण बन गया और सभी देखने वालों ने कहा कि हे परमेश्वर ! ऐसी सन्तान सभी को देना। उन्होंने अपने पिता जी की सेवा में घर पर ही वे सारे साधन एकत्रित कर लिए जो एक अच्छी गुणवत्ता वाले चिकित्सालय के आई०सी०यू० में होते हैं, दो डाक्टर लगाये जो एक एक करके दिन रात आवश्यक सेवा देते रहे, इसके साथ साथ पुत्र, पुत्रवधू तथा पुत्रियाँ बारी-बारी से हर समय पिता की सेवा में लगे रहे। परिवारी जनों का बस एक ही उद्देश्य था कि पिता जब तक रहें सुख से रहें। इस उदाहरण को बताने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह परिवार मेरे भी निकट है , मेरा यजमान परिवार है उनका नाम है श्री रविन्द्र सिंह चौहान। इनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि सदा सुखी रहें, हमेशा वेद मार्ग के अनुगामी रहें।
२. दूसरा उदाहरण नेपाल का है – इस उदाहरण को पढ़कर आप कहेंगे कि हे प्रभो ऐसी सन्तान किसी को नही देना। नेपाल के एक चिकित्सालय में एक फोन आता है कि नौकर के साथ के एक वृद्ध व्यक्ति आरहे हैं उनकी चिकित्सा कीजिए । चिकित्सक वृद्ध व्यक्ति का उपचार आरम्भ कर देते हैं अवस्था कुछ ऐसी थी उनकी दो दिन बाद मृत्यु हो गयी । ध्यान देने की बात यह है जिसने चिकित्सालय में वृद्ध का उपचार कराने के लिए फोन किया था वह उन वृद्ध का बेटा ही है लेकिन देखने तक नहीं आता है और अपने पिता की मृत्यु के बाद भी डाक्टर को फोन पर कहता है कि इनकी अन्त्येष्टि भी करा देना हम आपको उसका भी पैसा देदेंगे।
समाज में संस्कार हीनता बढ़ती जा रही है इसके बढ़ते अभी और अधिक भयानक परिमाण सामने आयेंगे। समाज में नैतिकता का वातावरण तैयार करने के लिए केवल संस्कार की साधन हैं।
आइये फिर हम अपने प्रसंग पर आते हैं – एक दिन शरीर को छोडकर आत्मा जब चला जाता है तब दो प्रश्न उपस्थित होते हैं कि आत्मा कहां गया? और इस मृत शरीर का क्या करें? ( आत्मा अपने कर्मों के आधार पर परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में आगे गति करता है या तो नये शरीर को प्राप्त करता है या मुक्ति में चला जाता है। जिसकी चर्चा आगे करेंगे ।) मृत शरीर के लिए वेद में आदेश है – भस्मान्तं शरीरं (यजु०) मृत शरीर का अन्त्येष्टि कर्म करना होता है इसे ही नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग, पुरुषयाग तथा दाह कर्म कहते हैं। मृत शरीर को अग्नि में रख दिया जाता है और अग्नि इस शरीर के सभी पांचों तत्वों (अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश) को अलग अलग कर देती है । अग्नि अपना भाग ले लेती है, जल वाष्प बनाकर अलग कर देती है , वायु का भाग वायु में मिल जाता है, आकाश का भाग आकाश में मिल जाता है तथा जो पड़ा रह जाता है वह भूमि का भाग है इसीलिए प्राचीन काल में अस्थियों को भूमि में गाड़ा जाता था । अस्थियों को नदियों में विसर्जित करना कुप्रथाहै। इसीलिए एक बात समाज में प्रचलित है कि अमुख व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया ।
अस्थियों से आत्मा का अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा जाता है। अस्थियों के नदी में विसर्जित करने से आत्मा की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आत्मा तो अपने कर्मों के आधार पर आगे की गति करता है । यदि ऐसा हो कि केवल अस्थियों के नदियों में विसर्जित करने से ही मुक्ति मिल जाय तो किये गये कर्मों का क्या औचित्य रह जायेगा।
आध्यात्मिक चर्चाओं में शरीर को ऋषि, मुनि और विद्वानों ने अनेक तरह से समझाया है। पिछली चर्चा में हमने समझा कि यमाचार्य शरीर को आत्मा का रथ कहते हैं। आज हम समझेंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज शरीर को वस्त्र की तरह समझाते हैं।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।
जगत में जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्यान्य नवीन शरीरों को प्राप्त करता है।
आइये इस प्रसंग को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम यह समझें कि वस्त्र बदलना बहुत आसान सा लगता है और शरीर बदलना बहुत कठिन लगता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति हो कि कोई गरीब व्यक्ति हो और उसके पास केवल एक जोड़ी ही वस्त्र हों तो उससे उसके वस्त्र उतारने को कहा जाय तो वह नहीं उतारेगा और यदि उससे यह कहा जाय कि इन वस्त्रों को उतार दो, आपको अच्छे और नये वस्त्र पहनने को देंगे तो वह बिना देर लगाये उतार देगा। शरीर बदलने में भी ठीक ऐसी ही स्थिति होती है – एक सामान्य व्यक्ति को शरीर बदलना (छूटना) बहुत ही कठिन कार्य लगता है लेकिन योगी को शरीर बदलना बहुत सरल और सहज लगता है क्योंकि योगी जीवन की यथार्थता से अच्छे से परिचित होता है।
योगी जानता है कि जैसे किसी रंग मंच पर अभिनय करने वाले वस्त्र बदलकर आते रहते हैं और अभिनय करते रहते हैं ठीक ऐसे ही संसार भी तो एक रंग मंच जैसा ही है जहां आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलकर आती रहती है और अपना एक जीवन अभिनय की तरह ही जी कर फिर आगे की यात्रा करती है।
इस प्रसंग को अच्छे से अध्ययन करें तो हम समझेंगे कि बड़ी समानता है रंग मंच और संसार में । एक नाटक मण्डली होती है और उसका एक मालिक होता है। और वह मालिक योग्यता अनुसार किसी को राजा, किसी को रानी, किसी को मन्त्री और किसी को सेवक बनाता है। मालिक कहीं तो झरोखे से देखता रहता है कि मेरी मण्डली के सदस्य कैसा अभिनय कर रहे हैं ।
हो सकता है नाटक करने वालों में से किसी ने मरने का नाटक किया हो। या तो पर्दा गिरते ही वह स्वयं उठाकर पीछे चला जाता है या उसे कुछ लोग उठा कर ले जाते हैं और पर्दे के पीछे कर देते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि जो रंग मंच पर मरा वह मरा नही केवल मरने का नाटक कर रहा था , वह पर्दे के पीछे चला गया केवल वस्त्र बदलने के लिए वह फिर से किसी अन्य अभिनय में दिखाई देगा।
इसी प्रकार यह संसार भी एक मण्डली जैसा है इस संसार का मालिक परमपिता परमात्मा है। परमात्मा ही सभी को उनके कर्मों के आधार पर शरीर प्रदान करता है और अन्तः करण में बैठा हुआ सभी के कर्मों को देखता रहता है।
संसार में जब कोई मरता है तो रंग मंच की तरह ही वह मरता नही है ( आत्मा अमर है) बल्कि पर्दे के पीछे चला जाता है वस्त्र बदलने के लिए ( पुनः नया शरीर आत्मा को प्राप्त होता है)।
यदि ऐसा हो कि रंग मंच पर जिसे राजा बनाया था उसने यदि अपना अभिनय ठीक से नही किया तो क्या मण्डली का मालिक फिर उसे राजा बनायेगा? तो आपका उत्तर होगा कि मण्डली का मालिक ऐसे व्यक्ति को फिर से राजा नहीं बनायेगा। ठीक ऐसे ही जीवात्मा मनुष्य शरीर पाकर यदि मानवता से जीवन नहीं जीता है तो परमेश्वर फिर उसे अन्य योनियों में भेज देता है।
जैसे रंग मंच पर अभिनय करना अच्छे से आना चाहिए तभी अभिनय सफल होगा ठीक इसी प्रकार संसार में जीवन जीना आना चाहिए तभी जीवन सफल होगा।
जीवन को समझने के लिए यजुर्वेद में बड़ा सुन्दर उपदेश है –
अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता।
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुचम्।।
हे जीवो! जिस जगदीश्वर ने (अश्वत्थे) कल ठहरेगा वा नहीं ऐसे अनित्य संसार में (वः) तुम लोगों की (निषदनम्) स्थिति की (पर्णे) पत्ते के तुल्य चञ्चल जीवन में (वः) तुम्हारा (वसतिः) निवास (कृता) किया (यत्) जिस (पुरुषम्) सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को (किल) ही (सनवथ) सेवन करो उसके साथ (गोभाजः) पृथिवी वाणी इन्द्रियाँ वा किरणों का सेवन करने वाले (इत्) ही तुम लोग प्रयत्न के साथ धर्म में स्थिर (असथ) होओ।
अर्थात् मनुष्यों को चाहिए कि अनित्य संसार में शरीरों और पदार्थों को प्राप्त हो के क्षणभंगुर जीवन में धर्माचरण के साथ नित्य परमात्मा की उपासना कर आत्मा और परमात्मा के संयोग से उत्पन्न हुए नित्य सुख को प्राप्त हों।
इस मन्त्र का एक सन्देश यह है कि जिस संसार में हम बैठे हैं उसका पता यह नहीं है कि यह कल तक रहेगा या नहीं। कहीं भी भूकम्प, बाढ़, तूफान आता है जिससे पहले लोग यह सोचते है अभी तो बहुत समय तक रहेंगे लेकिन थोड़ी ही देर में कितने ही प्राणी काल के कराल गाल में समा जाते हैं।
भूकम्प आदि ही नही बल्कि सामान्य जीवन जीते हुए भी पता नही कब सोते सोते , चलते चलते या बैठे बैठे ही जीवन समाप्त हो जाये।
इस मन्त्र का दूसरा सन्देश है कि पत्ते के समान चञ्चल जीवन में तुम रह रहे हो। पत्ते पर पड़ी ओस आदि की बूंद का क्या पता कब लुढक पड़े । ओस की बात छोड़िये पत्ते का भी तो ठिकाना नहीं है कि वह कब तरु से टूट जाये। सामान्यतया पत्ते की तीन दशायें होती हैं – निकलते समय वह जब कोपल कहलाता है तब अरुणिमा लिए होता है फिर यह कोपल कुछ बड़ी होती है कुछ सख्त होती है और इस पर हरियाली आती है कुछ समय हरियाली के बाद पीलापन आने लगता है और पूरा पीला होने के बाद सदैव के लिए डाल से बिछुड़ जाता है । ठीक ऐसे ही मनुष्य का भी जीवन होता है, कोपलों की तरह मासूम बचपन होता है तथा हरी सख्त पत्तियों की तरह युवावस्था आती है और पीली पत्तियों की तरह वृद्धावस्था आती है और पतझड़ की तरह मृत्यु होती है।
यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि केवल वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी ऐसा नही है अरे जब हवा अधिक तेज होती है तो वह कोपलों और सख्त पत्तियों को भी डाल पर नहीं रहने देती इसी प्रकार मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। इसीलिए वेद ने उपदेश दिया है कि वक्त रहते परमेश्वर का ध्यान करना चहिए।
महाभारत में पितामह भीष्म ने अपने जीवन की सन्ध्या वेला में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया –
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युः कालो भविष्यति।
युवैव धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्।।
अर्थात् हे युधिष्ठिर! किसी को कुछ नहीं पता कि कब किसका कहां मृत्यु समय आ पहुंचेगा। अतः इस सत्य को समझ कर युवावस्था में ही धर्माचरण करो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं ।
इस विषय में नीतिकार ने कहा –
यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः।
तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति।।
अर्थात् जब तक यह शरीर स्वस्थ बना हुआ है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया है तभी तक आत्म-श्रेयस् का कुछ कार्य कर डालो, प्राणान्त होने पर क्या कर सकोगे?
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः |
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ||
अर्थात् मनुष्य का शरीर नश्वर है, और धन वैभव भी शाश्वत नहीं होता है । मृत्यु सदैव हमारे साथ रहती है (मृत्यु कभी भी हो सकती है) । अतः हमारा यह कर्तव्य है कि धर्म द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन कर पुण्य प्राप्त करें ।
एक कवि कहता है –
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली।
मलयाचल सेवित शीतल मन्द सुगन्ध समीर मिली न मिली ।।
कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली ।
जपले प्रभु नाम अरी रसना फिर अन्त समय में हिली ना हिली ।।
योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज का उपदेश है –
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि।।
जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिये।।
जन्म मृत्यु का होना अपरिहार्य है वैसे ही जैसे प्रातःकाल होता है फिर दोपहर होता है फिर साम होती है और फिर रात आती है और फिर प्रातःकाल होता है, इस क्रम को रोका नहीं जा सकता है, बदला नही जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जन्म होता है फिर युवावस्था आती है फिर वृद्धावस्था आती है और फिर मृत्यु होती है और फिर जन्म होता है यह क्रम को भी रोका नहीं जा सकता, बदला नही जा सकता है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि मृत्यु पर शोक मत करो।
इस प्रसंग को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति दिन में रात्रि आने को लेकर चिन्ता करे और कहे कि हाय हाय रे रात आयेगी तो उसका चिन्ता करना व्यर्थ ही है क्योंकि रात तो आयेगी ही, इसीप्रकार कोई यह कहें कि हाय हाय रे कल का दिन होगा तो भी चिन्ता करना व्यर्थ ही है क्योंकि कल का दिन तो आयेगा ही। इस पर चिन्ता नही करनी चाहिए बल्कि इस पर चिन्तन करना चाहिए कि अभी रात आने में समय है और जो भी समय रात आने में है उसे सार्थक व्यतीत किया जाय। इसी प्रकार कल का दिन तो होगा यह चिन्ता का विषय नही है बल्कि अगला दिन अच्छा कैसे हो यह चिन्तन का विषय है।
ठीक इसीप्रकार मृत्यु शोक या चिन्ता का विषय नहीं है क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, होनी ही है, चिन्तन का विषय तो यह है कि मृत्यु तक हमारे पास जो भी समय है उसे सार्थक व्यतीत किया जाय। तथा अगला जन्म चिन्ता का विषय नही है क्योंकि वह तो होना ही है, हमें इस बात पर चिन्तन करना चाहिए कि अगला जन्म मनुष्य का श्रेष्ठता से युक्त मिलना चाहिए।
“आज के मनुष्य का चिन्तन बदल गया है जिस विषय पर चिन्तन करना चाहिए उस पर तो चिन्तन नही करता है और जिस विषय पर चिन्तन नहीं करना चाहिए उस पर चिन्तन करता है।”
ऋषि और महर्षियों ने जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चिन्तन किया, जीवन को सफल बनाने के लिए अध्ययन किया और मोक्ष के लिए साधना की। संसार का मार्गदर्शन भी किया। (इस पर विस्तार से आगे लिखेंगे)
अभी तक हमने समझा कि –
० आत्मा एक अविनाशी और अनादि सत्ता है।
० शरीर पाँच तत्वों से मिलकर बनता है और अन्ततः उन्हीं पाँच तत्वों में विलीन हो जाता है।
० शरीर और आत्मा का संयोग जन्म है, शरीर और आत्मा का साथ-साथ चलना जीवन है तथा शरीर और आत्मा का वियोग ही मृत्यु है।
० जन्म और मृत्यु का होना अनिवार्य है अर्थात् आत्मा का शरीर में आना और शरीर को छोड़ना निश्चित है।
० यहां एक बात और जानना आवश्यक है कि इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में तीन अनादि सत्तायें हैं – परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति । इस प्रसंग को क्रमशः और विस्तार से पढ़ने लिए ब्लॉग ( shankaragra.blogspot.com ) पर सैद्धान्तिक चर्चा पढ़ें।
आगामी चर्चा में विस्तार से लिखा जायेगा कि जन्म , मृत्यु और जीवन का आधार क्या है? कारण क्या है?
हमारे जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख-दुःख का आधार कर्म है ।
समाज में प्रचलित विभिन्न विचार धाराओं का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि आज का समाज वैचारिक प्रदूषण में बहुत गहराई तक फस गया है। इसीलिए जीवन की सफलता का आधार कर्म/पुरुषार्थ को न मानकर अन्य साधनों को मान रहा है। वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार हमारे जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख-दुःख का आधार /कारण कर्म है। लेकिन समाज में ऐसा भी प्रचार किया गया है कि हमारे जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख:दुःख का आधार परमेश्वर, काल या तन्त्र-यन्त्र आदि हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा तो परमेश्वर की कठपुतली है, परमेश्वर ही आत्मा से कर्म कराता है । इसीलिए सुख – दुःख आदि सब परमेश्वर के आधीन है।
उपरोक्त मान्यता पर महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक सिद्धान्त लिखते है कि आत्मा कर्म करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र है फल भोगने के लिए नहीं । अर्थात् आत्मा परमात्मा की कठपुतली नहीं हैं, परमात्मा आत्मा से कर्म नहीं कराता है बल्कि आत्मा स्वतन्त्रता से कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप सुख-दुःख आदि प्राप्त करता है।
कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ समय के आधीन है, कलियुग चल रहा है इसीलिए बुरे कर्म बढ़ रहे हैं।
इस मान्यता को समझने के लिए वैदिक सिद्धान्त समझना पड़ेगा, वैदिक सिद्धान्त के अनुसार समय कोई कर्म नहीं कराता है अर्थात् कर्म के लिए समय कारण नहीं है । समय के बारे में वेद में कहा है –
कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि: सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता: ।
तमारोहन्ति कवयो वियश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ।। (अथर्ववेद १९/५२/१)
(सप्तरश्मिः) सात प्रकार की किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान, (सहस्राक्षः) सहस्रों नेत्र वाला, (अजरः) बूढ़ा न होने वाला, (भूरिरेताः) बड़े बल वाला, (कालः) काल [समय रूपी] (अश्वः) घोड़ा ( वहति) चलता रहता है। (तम्) उस पर (कवयः) ज्ञानवान (विपश्चितः) बुद्धिमान लोग (आरोहन्ति) चढ़ते हैं, (तस्य) उस [काल] के (चक्रा) चक्र [चक्र अर्थात् घूमने के स्थान] (विश्वा) सब (भुवनानि) सत्ता वाले हैं।
अर्थात् (काल) समय सब देखता है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी बूढ़ा (कमजोर) नही होता, बलवान घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। जैसे घोड़े को बुद्धिमान लोग आगे से पकड़कर सवारी करते हैं वैसे ही बुद्धिमान लोग समयानुसार कार्यों को करके जीवन सफल बनाते हैं।
काल गणना के लिए छोटी-बड़ी अनेक इकाइयां है उनमें से कलियुग भी समय मापने की बड़ी इकाई है। जो कि समय नापने में उपयोग की जाती हैं ।
भारतीय प्राचीन काल गणना –
२ परमाणु = १ अणु
३अणु = १ त्रिसरेणु
३ त्रिसरेणु =१ त्रुटि (३ त्रिसरेणु को पार करने मे सूर्य को लगा समय १त्रुटि)
१०० त्रुटि = १ वेध
३ वेध = १ लव
३ लव = १ निमेष
३ निमेष = १ क्षण
५ क्षण = १ काष्ठा
१५ काष्ठा = १ लघु
१५ लघु = १ दण्ड
२ दण्ड = १ मुहुर्त
३ मुहूर्त = १ प्रहर
४ प्रहर = १ दिन
१ दिन रात = १ अहोरात्र
१५ अहोरात्र = १ पक्ष
२ पक्ष = १ मास
१२ मास = १ वर्ष
४३२००० वर्ष = १ कलियुग
८६४००० वर्ष = १ द्वापर युग
१२९६००० वर्ष = १ त्रेता युग
१७२८००० वर्ष = १ सतयुग
४३२०००० वर्ष = १ चतुर्युगी
७१ चतुर्युगी = १ मन्वन्तर
१४ मनवन्तर + छः चतुर्युगी = १ कल्प = १ ब्रह्मदिन = सृष्टिकाल = ४३२००००००० वर्ष
वर्तमान में सृष्टि का सातवें वैवस्वत मनवन्तर का २८ वें कलियुग का ५१२० वां वर्ष चल रहा है, अर्थात् १९६०८५३१२० वां चल रहा है ।
इस गणना के आधार पर ४५४ वां कलियुग चल रहा है । युग भी वार और महिनों की तरह की बदलते रहते हैं। समय सुख/दुःख के लिए कारण नहीं होता है ।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सुख- दुःख आदि सब तन्त्र-यन्त्र, टोने-टोटके, झाड़-फूंक, डाकिनी-साकिनी, भूत-प्रेत, मूर्ति पूजा आदि से मिलता है। लेकिन ये लोग यह विचार कभी नहीं करते कि वे लोग सुखी क्यों हैं जो इन मान्यताओं पर विस्वास नहीं करते।
उपरोक्त बात को समझने के लिए केवल एक तर्क (दलील) यहां देते हैं सम्भव है उससे कुछ स्पष्ट हो जाय। – एक ही कक्षा के दो विद्यार्थी लिए जायें और एक विद्यार्थी इनको दे दिया जाय जो तन्त्र-यन्त्र, टोने-टोटके, झाड़-फूंक, डाकिनी-साकिनी, भूत-प्रेत, मूर्ति पूजा पर पूरा विस्वास करते हैं और इनसे कहा जाय कि आप इस विद्यार्थी पर तन्त्र – यन्त्र और मूर्ति पूजा आदि वर्षभर कराइए लेकिन पढ़ाना नही है और वर्ष के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण करके दिखाइए। और दूसरे विद्यार्थी को मूर्तिपूजा आदि से बिल्कुल दूर रखिये वर्षभर ठीक से पढ़ाइए और उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण करके दिखाइए। अब आप समझ गये होंगे कि सफलता आदि सुख का आधार पुरुषार्थ ही है तन्त्र आदि नहीं।
देखिए कैसा अन्धविश्वास चल रहा है जिस देश में “श्रीयन्त्र” कुछ ही रुपयों में मिल रहा हो वहां धन के लिए पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है बस श्रीयन्त्र घर में रख दीजिए और धन आ ही जायेगा । ऐसे ही समाज में बहुत भ्रम नित्य प्रचारित किये जारहे है।
इस चर्चा में हमने समझने का प्रयास किया कि समाज में अनेक अवैदिक मान्यताओं का प्रचार हुआ है जिससे समाज भ्रमित हो गया है।
अगली चर्चा में हम समझेंगे कि हमारे जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख-दुःख का आधार कर्म है ।
हमारे जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख-दुःख का आधार कर्म है ।
इसीलिए वेद कर्म करने का उपदेश करता है –
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। ( यजुर्वेद )
मनुष्य (इह) इस संसार में (कर्माणि) धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को (कुर्वन्) करता हुआ (एव) ही ( शतम्) सौ (समाः) वर्ष (जिजीविषेत्) जीवन की इच्छा करे (एवम्) इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म में प्रवर्तमान (त्वयि) तुझ (नरे) व्यवहारों को चलानेहारे जीवन के इच्छुक होते हुए (कर्म) अधर्मयुक्त अवैदिक काम्य कर्म (न) नहीं ( लिप्यते) लिप्त होता (इतः) इस से जो ( अन्यथा) और प्रकार से (न, अस्ति) कर्म लगाने का अभाव नहीं होता है।
अर्थात् मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखनेहारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्पमृत्यु को हटावे, युक्त आहार विहार से सौ वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या, अवस्था और सुशीलता बढ़ती है।
शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम्।
कर्मजा गतयो नॄणामुत्तमाधममध्यमाः।। ( मनु० )
( मनः वाक्-देह संभवम् कर्म ) मन, वचन और शरीर से किये जाने वाले कर्म ( शुभ-अशुभ-फलम् ) शभ-अशुभ फल को देने वाले होते हैं ( कर्मजा-नॄणाम् ) और उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की ( उत्तम-अधम-मध्यमाः गतयः ) उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन गतियां=जन्मवस्थायें होती हैं।
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । ( योगदर्शन )
(मूले) मूलकारण के (सति) विद्यमान होने पर ही (तद्विपाक:) पुण्य-पाप रूप कर्माशय का फल (जात्यायुर्भोगा:) जन्म, आयु तथा भोग होता है।।
जन्म का नाम “जाति”
जीवनकाल का नाम “आयु”
और सुख दुःख के हेतु शब्दादि विषयों की प्राप्ति का नाम “भोग” है,
यह तीनों पुण्य-पाप रूप कर्माशय का फल होने से “कर्मविपाक” कहलाते हैं।।
उपरोक्त प्रमाणों से आप समझ ही गये होंगे कि सम्पूर्ण जीवनों का आधार कर्म ही है। इसीलिए वेद कर्म करने का आदेश देता है, लेकिन यहां ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने संसार को निकम्मा बनने का उपदेश किया है ,जिसकी चर्चा आगामी लेख में करेंगे।
पिछली चर्चा में हमने समझा कि हमारे जन्म, मृत्यु, जीवन और सुख-दुःख का आधार कर्म है । इसीलिए वेद और वैदिक साहित्य कर्म करने का उपदेश करता है।
योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज कर्म के सन्दर्भ में उपदेश करते हैं –
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।
( कर्मणि ) कर्म में ( एव ) ही ( अधिकारः ) अधिकार ( ते ) तेरा ( मा ) न कि ( फलेषु ) फलों में ( कदाचन ) कभी भी या कतई ( मा ) मत/नहीं ( कर्मफलहेतुः ) कर्म के फलों का कारण ( भूः ) होवो ( मा ) मत/नहीं ( ते ) तेरा ( सङ्गः ) संग/साथ ( अस्तु ) हो ( अकर्मणि ) अकर्म में।
अर्थात् तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं।
ध्यान दीजिए – यहां कहा गया है कि कर्म में अधिकार है फल में नहीं । क्योंकि फल तो परमेश्वर प्रदान करेगा। भावार्थ में हम यह भी समझ सकते हैं कि फल तो निश्चित मिलेगा ही इसीलिए कर्म कीये जा। यहां यह भी स्पष्ट किया है कि कहीं इसका अर्थ यह न लेना कि जब फल में अधिकार नहीं तो ( अकर्म ) कर्म भी ना करें । अर्थात् अकर्म से तेरा काम नही चलेगा कर्म ही एक कल्याण का पथ है।
कर्मणा जायते सर्वं कर्मैव गति साधनम्।
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत।। (वि०पु०)
कर्म द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होता है और कर्म ही आगे बढ़ने का साधन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अच्छा कर्म ही करे।
गोस्वामी तुलसीदास जी अनेक स्थानों पर कर्म को ही जीवन का आधार लिखते है लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विरोधी भी लिखते हैं। इस तरह की विरोधी विचारधारा से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों में अकर्मण्यता आती है।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा । जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥
सकल पदारथ हैं जग मांही। कर्म हीन नर पावत नाहीं।।
उपरोक्त विचारों में कर्म का वैदिक सिद्धान्त है । संसार में कर्म ही प्रधान है , कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। संसार में सब कुछ कर्मों से ही प्राप्त होता है अकर्मण्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
ध्यान दीजिए – निम्नलिखित चौपाई से उपरोक्त सिद्धान्त का विरोध होता है –
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा॥
जो कुछ राम ने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा (विस्तार) बढ़ावे।
इस प्रकार के विरोधी विचारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। जिनसे अकर्मण्यता बढ़ती है।
आइये ऐसे ही कुछ विचारों को आपके सम्मुख रखते हैं। आप स्वयं यह विचार कीजिए कि इन विचारों से समाज कर्मशील बनेगा या अकर्मण्य बनेगा।
तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए।
अनहोनी होनी नही, होनी हो सो होए॥
तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम पर विश्वास करके आराम करो, इस संसार में कुछ भी अनहोनी नहीं होगी और जो होना उसे कोई रोक नहीं सकता।
क्या संसार में चोरी, व्यभिचार और अत्याचार होना ही था ?
और क्या इन अपराधों को रोका जा सकता है ?
यदि हम तुलसीदास जी की बात मानें तो अत्याचार और बढ़ेगा और वैदिक कर्म दर्शन को समझ लें तो अत्याचार को रोकने का पुरुषार्थ किया जायेगा।
अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम,
दास मलूका कह गए सब के दाता राम
अजगर को किसी की नौकरी नहीं करनी होती और पक्षी को भी कोई काम नहीं करना होता, ईश्वर ही सबका पालनहार है, इसलिए कोई भी काम मत करो ईश्वर स्वयं देगा। आलसी लोगों के लिए श्री मलूकदास जी का ये कथन बहुत ही उचित है।
उपरोक्त विचारों को अच्छे से अध्ययन करने के बाद सारांश में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि कर्म ही जीवनों का आधार है। अवैदिक प्रदूषित विचारों से व्यक्ति का अकर्मण्य और अत्याचारी होना निश्चित है। वैचारिक क्रान्ति के लिए वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार होना आवश्यक है।
आगे के लेख में हम विस्तार से लिखेंगे –
कर्म क्या है ?
कर्म कौन करता है ?
कर्म के साधन ?
कर्म कैसे होता है ?
कर्म के प्रकार ?
कर्म के परिणाम-प्रभाव-फल ?
पिछली चर्चाओं में हमने समझा कि कर्म ही जीवन आदि सभी भोगों का आधार है । इसीलिए अब हम कर्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे ।
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज आर्योद्देश्यरत्नमाला में कर्म की परिभाषा लिखते हैं – “जो मन, इन्द्रिय और शरीर से जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहाता है। वह शुभ , अशुभ और मिश्रित भेद से तीन प्रकार का होता है।”
महाराज मनु ने कर्म दर्शन को एक ही श्लोक में समायोजित किया है –
शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम्।
कर्मजा गतयो नॄणामुत्तमाधममध्यमाः।।
( मनः वाक्-देह संभवम् कर्म ) मन, वचन और शरीर से किये जाने वाले कर्म ( शुभ-अशुभ-फलम् ) शुभ-अशुभ फल को देने वाले होते हैं ( कर्मजा-नॄणाम् ) और उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की ( उत्तम-अधम-मध्यमाः गतयः ) उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन गतियां=जन्मवस्थायें होती हैं।
उपरोक्त प्रमाणों से हमने समझा कि –
० जीव ( आत्मा ) कर्म करता है।
० जीव के कर्म करने साधन है – मन, वाणी और शरीर।
० कर्म तीन प्रकार के होते है – शुभ, अशुभ और मिश्रित।
० कर्मों के आधार पर ही सभी जीवों को तीन प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं – उत्तम, मध्यम और अधम।
जीव ( आत्मा ) कर्म कैसे करता है ? यह जानने के लिए कठोपनिषद् में उल्लेख किया है –
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।।
इस जीवात्मा को तुम रथी, रथ का स्वामी, समझो, शरीर को उसका रथ, बुद्धि को सारथी, रथ हांकने वाला, और मन को लगाम समझो ।
इंद्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।।
मनीषियों, विवेकी पुरुषों, ने इंद्रियों को इस शरीर-रथ को खींचने वाले घोड़े कहा है, जिनके लिए इंद्रिय-विषय विचरण के मार्ग हैं, इन्द्रियों तथा मन से युक्त इस आत्मा को उन्होंने भोग करने वाला बताया है ।
अर्थात् आत्मा जब कुछ कर्म करती है तो बुद्धि द्वारा मन को प्रेरित करती है और मन इन्द्रियों से काम लेता है। मन ज्ञानेन्द्रियों से जुड़ता है तो विषयों को बुद्धि तक पहुँचाने का काम करता है और जब कर्मेन्द्रियों से जुड़ता है तो कर्म कराता है।
वर्णोच्चारण शिक्षा में एक प्रसंग है। जिसमें आत्मा बोलने के लिए मन और इन्द्रियों से कैसे काम लेता है ऐसा वर्णन है।
आत्मा बुद्ध् या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।
मारुतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्।।
जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता, विद्युतरूप जाठराग्नि को ताड़ता, वह वायु को प्रेरणा करता, और वायु उरःस्थान में विचरता हुआ मन्द स्वर को उत्पन्न करता है।
अर्थात् आत्मा जब कुछ कहना चाहती है तो बुद्धि पूर्वक मन को नियुक्त करती है और मन अग्नि को प्रेरित करता है और अग्नि वायु को प्रेरित करता है और वायु कण्ठ आदि स्थानों से निकलता हुआ स्वर उत्पन्न करता है। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है जब वायु मुख से विचरण करता है तो मन उस समय मुख के उच्चारण स्थानों को भी व्यवस्थित करता है अर्थात् कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ और नासिका स्थानों से वायु विचरण करता है। जब हम ‘क’ उच्चारण करते हैं तो कण्ठ से और ‘प’ उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ से ही उच्चारण होता है। इस विषय को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हारमोनियम के प्रयोग से समझ सकते हैं। जैसे हारमोनियम से स्वर निकलते हैं वैसे ही हमारे मुख में से स्वर निकलते हैं । हारमोनियम में एक हाथ से वायु भरी जाती हैं और दूसरे हाथ की अंगुलियों से स्वर निकाले जाते हैं । यह सब भी बुद्धि और मन से युक्त होकर ही सम्भव है।
यहां हमने समझा कि आत्मा बुद्धि से युक्त होकर मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है। आगे हम समझेंगे आत्मा इन मन आदि साधनों से कितने प्रकार के कर्म करता है।
कर्म करने वाला आत्मा है और यह आत्मा मन, वाणी और शरीर से कर्म करता है। मुख्यतः कर्म दो प्रकार के होते हैं – सकाम और निष्काम ।
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के वेद विषय प्रकरण में परिभाषा लिखते हैं – “सब दुःखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत् करना, यही ‘निष्काम’ मार्ग कहाता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती, इसी कारण से इसका फल अक्षय है। और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किये जाते हैं , उसको ‘सकाम’ कहते हैं, इस हेतु से इसका फल नाशवान् होता है, क्योंकि सब कर्मों करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता।” अर्थात् सकाम कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो लौकिक फल ( धन , पुत्र , यश आदि ) को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते है । तथा निष्काम कर्म वे होते है , जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किए जाए बल्कि ईश्वर / मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए जाएं ।
सकाम और निष्काम का विस्तार से अध्ययन करें तो कर्म चार प्रकार के होते हैं। योग दर्शन में कहा है –
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्।। (४/७)
योगी के कर्म अशुक्ल = लौकिक पुण्य फल की कामना से रहित और अकृष्ण = पाप रहित होते हैं अर्थात् ईश्वरप्राप्तिमात्र के लिये किये गये ‘निष्काम कर्म’ होते हैं। योगी से भिन्न सांसारिक व्यक्तियों के शुभ, अशुभ और मिश्रित तीन प्रकार के कर्म होते हैं।
यहां योगदर्शनकार ने कर्मों के चार प्रकार के विभाग किये हैं –
१. शुक्ल
२. कृष्ण
३. शुक्ल-कृष्ण (मिश्रित)। और
४ अशुक्ल अकृष्ण।
० पुण्य कर्म को ‘शुक्ल’ कहते हैं।
० पाप कर्म को ‘कृष्ण’ कहते हैं।
० पुण्य-पाप मिश्रित कर्म को ‘शुक्लकृष्ण कहते हैं।
(उपरोक्त तीनों सकाम कर्म हैं।)
० निष्काम कर्म को ‘अशुक्ल-अकृष्ण’ कहते हैं।
जो अपने और अन्यों के लिए लौकिक सुख को देते हैं , वे शुक्ल कर्म हैं। जैसे उत्तम कार्यों के लिए दान देना, निर्बलों की रक्षा करना आदि।
जो अपने और अन्यों के लिए दुःखप्रद होते हैं, वे कृष्ण कर्म हैं। जैसे चोरी करना, अन्याय करना आदि।
जो कर्म सुखप्रद और दुःखप्रद होते हैं वे शुक्लकृष्ण (मिश्रित) कर्म होते हैं। जैसे खेती करना, विविध बांधो का निर्माण करना आदि। क्योंकि इन कार्यों में अनेक प्राणियों को सुखदुःख दोनों की प्राप्ति होती है।
इन कर्मों को ऐसे भी समझना चाहिए – शुक्ल कर्म जिन्हें शुभ कर्म भी कहते हैं और कृष्ण कर्म जिन्हें अशुभ कर्म भी कहते हैं।
शुभ कर्म = शुक्ल = पुण्य = सत्कर्म = धर्म
अशुभ = कृष्ण = पाप = दुष्कर्म = अधर्म
शुभ कर्म – जिन कर्मों से स्वयं को और दूसरों को सुख मिले।
अशुभ कर्म – जिन कर्मों से स्वयं को और दूसरों को दुःख मिले।
इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कर्म ईश्वर की आज्ञानुसार हैं वे शुभ कर्म हैं और
जो ईश्वराज्ञा के विरुद्ध हैं वे अशुभ कर्म हैं।
शुभ और अशुभ कर्मों को अच्छे से समझने के लिए यहां विस्तार से वर्णन किया जारहा है।
अशुभ कर्म – महाराज मनु ने मन, वाणी और शरीर के अशुभ कर्मों का वर्णन किया है।
० मन के तीन अशुभ (कृष्ण) कर्म होते हैं-
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्।
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्।।
( मानसं कर्म त्रिविधम् ) मन से चिन्तन किये गये अधर्म = अशुभ फलदायक कर्म तीन हैं – ( परद्रव्येषु + अभिध्यानम् ) दूसरे के धन, पदार्थ आदि को अपने अधिकार में लेने का विचार रखना, ( मनसा + अनिष्ट चिन्तनम् ) मन में किसी का बुरा करने का समय सोचना, ( च वितथ + अभिनिवेशः ) मिथ्या विचार या संकल्प करना, मिथ्या विचार या सिद्धान्त को सत्य स्वीकार करना।
० वाणी के चार अशुभ (कृष्ण) कर्म होते है-
पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः।
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्।।
( वाङ्मयं चतुर्विधं स्यात्) वाणी के अधर्म = अशुभ फलदायक कर्म चार प्रकार के ये हैं – ( पारुष्यम् ) कठोर वचन बोलकर किसी को कष्ट देना, ( च ) और ( अनृतम् ) झूठ बोलना, ( पैशुन्यम् अपि सर्वशः ) किसी की किसी भी प्रकार की चुगली करना, ( च ) और ( असम्बद्ध प्रलापः ) किसी पर मिथ्या लांक्षन या बुराई लगाना अथवा ऊल-जलूल बातें करना, अफवाहें उड़ाना आदि।
० शरीर के तीन अशुभ ( कृष्ण ) कर्म होते हैं-
अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम्।।
( शारीरंत्रिविधं स्मृतम् ) शरीर से किये जाने वाले अधर्म = अशुभ फलदायक कर्म तीन प्रकार के माने हैं – ( अदत्तानाम् उपादानम् ) किसी के धन या पदार्थों को स्वामी के दिये बिना चोरी, डकैती, रिश्वत आदि अधर्म के रूप में ग्रहण करना, ( च ) और ( अविधानतः हिंसा एव ) शास्त्र के द्वारा कर्तव्य के रूप में विहित हिंसाओं के अतिरिक्त हिंसा करना, [ शास्त्रविहित हिंसाएं हैं – युद्ध में शत्रु हिंसा करना, आततायी की हिंसा आदि ] ( च ) और ( परदारा + उपसेवा ) दूसरे की स्त्री से शारीरिक सम्बन्ध बनाना।
शुभ कर्म – अशुभ कर्मों के साथ महाराज मनु शुभ कर्मों का वर्णन धर्म के लक्षणों के रूप में करते हैं-
धृति: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।
( धृतिः ) कष्ट या विपत्ति में भी धैर्य बनाये रखना और दुःखी एवं विचलित न होना तथा धर्म पालन में कष्ट आने पर भी धैर्य रखकर पालन करते रहना, दुःखी होकर या विचलित होकर धर्म का त्याग न करना, ( क्षमा ) धर्म पालन के लिए निन्दा-स्तुति, मान-अपमान को सहन करना, ( दमः ) ईर्ष्या, लोभ, मोह, वैर आदि अधर्म रूप संकल्पों या विचारों से मन को वश में करके रखना,( अस्तेयम् ) चोरी, टकैती, झूठ, छल-कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्माचरण से किसी की वस्तु धन आदि न लेना, ( शौचम् ) तन और मन की पवित्रता रखना, ( इन्द्रियनिग्रहः ) इन्द्रियों को अपने अपने विषयों के अधर्म और आसक्ति से रोककर रखना, ( धीः ) बुद्धि की उन्नति करना, मननशील होकरबुद्धिवर्धक उपायों को करना बुद्धिनाशक नशा आदि न करना, ( विद्या ) सत्यविद्याओं की प्राप्ति में अधिकाधिक यत्न करके विद्या और ज्ञान की उन्नति करना, ( सत्यम् ) मन, वचन, कर्म से सत्य मानना, सत्य भाषण व सत्याचरण करना, आत्मविरुद्ध मिथ्याचरण न करना, ( अक्रोधः ) क्रोध के व्यवहार और बदले की भावना का त्याग कर शान्ति आदि गुणों को ग्रहण करना, ( दशकं धर्मलक्षणम् ) ये दश धर्म के लक्षण हैं । इन गुणों से धर्म पालन की पहचान होती है।
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज इनमें अहिंसा [ अहिंसा – सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ वैरभाव को छोड़कर प्रीति से वर्तना, अहिंसा है। ] को जोड़कर धर्म के ग्यारह लक्षण बताते हैं।
उपरोक्त ग्यारह लक्षण शुभ कर्म हैं, धर्म हैं, पुण्य कर्म हैं इनको धारण करने से, आचरण करने से ही सभी का हित होगा।
इन शुभ कर्मों को योग दर्शन में यम और नियम कहा है।
यम – अहिंसासत्यास्तरयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम हैं।
नियम – शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमां
शौच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ये नियम हैं।
इन शुभ कर्मों को ही तीर्थ ( तरने का साधन ) और मानव मूल्य कहते हैं। इन गुणों को धारण करके व्यक्ति मूल्यवान होता है।
प्राचीन वैदिक काल में इन शुभ गुणों को सभी धारण करते थे इसीलिए कहीं पर भी चोरी, डकैती, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं होता था। विश्वभर में आर्यावर्त को देवभूमि कहते थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने इन शुभ कर्मों का केवल उपदेश ही नहीं किया बल्कि स्वयं जीवन में भी धारण करके दिखा दिया । उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अनेकों अनुयायियों ने भी इन गुणों को धारण करके जीवन पवित्र बनाकर समाज का उपकार किया है। आइये इन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण करें। इससे ही विश्व का कल्याण होगा।
कर्म – मन, वाणी और शरीर से जीवात्मा जो विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे यज्ञ करना, सत्य बोलना, दान देना, सब के लिए सुख की कामना करना इत्यादि ।
कर्म का परिणाम – किसी भी क्रिया ( कर्म ) की निकटतम प्रतिक्रिया को ‘कर्म का परिणाम’ कहते हैं। जैसे –
कर्म – यज्ञ करना,
कर्म का परिणाम – वायु की शुद्धि, सुगन्ध प्राप्ति, स्वास्थ वृद्धि, रोग निवारण आदि।
कर्म का प्रभाव – कर्म, कर्म के परिणाम अथवा कर्म के फल को जानकर चेतनों पर जो इनकी प्रतिक्रिया होती है, उसे ‘कर्म का प्रभाव’ कहते हैं । जैसे –
कर्म – यज्ञ करना।
कर्म का प्रभाव – यज्ञ कर्ता को प्रसन्नता, आनन्द, शान्ति, उत्तम संस्कार बनना इत्यादि और जिन जिन मनुष्यों को यज्ञ-कर्ता के यज्ञ कर्म की सूचना मिलेगी वे सब मनुष्य यज्ञ कर्ता को अच्छा व्यक्ति मानेंगे और उन्हें यज्ञ के लिए प्रेरणा भी मिलेगी तथा उनकी यजमान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी।यह उन मनुष्यों पर पड़ने वाला यज्ञ कर्म का प्रभाव है।
कर्म का फल – कर्म करे अनुसार कर्म कर्ता को जो न्याय पूर्वक सुख दुःख या सुख दुःख के साधन प्राप्त होते हैं उन्हें कर्म का फल कहते हैं। जैसे –
कर्म – यज्ञ करना
कर्म का फल – यज्ञ कर्ता को पुनर्जन्म में अच्छे, धार्मिक, विद्वान, सदाचारी, सम्पन्न मातापिता के घर में मनुष्य जन्म प्राप्त होना, यज्ञ कर्म का फल है।
कर्म का परिणाम और प्रभाव कर्म के कर्ता पर भी हो सकता है अथवा अन्यों पर भी हो सकता है।
कर्म का फल न्यायपूर्वक कर्म कर्ता को ही मिलता है, अन्य को नहीं। कहीं कहीं सामूहिक कर्मों का सामूहिक फल भी होता है।
जहाँ किसी कर्म कर्ता के कर्म से किसी अन्य को अन्याय पूर्वक सुख दुःख मिलता है वह कर्म का फल नहीं है बल्कि वह कर्म का परिणाम या प्रभाव है।
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः।
( क्लेश-मूलः ) अविद्यादि क्लेश है मूल = कारण जिस कर्म समुदाय के वह ( कर्माशय ) कर्म समुदाय ( दृष्ट-अदृष्ट-जन्म-वेदनीयः ) वर्तमान तथा भावी जन्म में भोग्य = फल देनेवाले होते है।
इस सूत्र में इस जन्म में फल देने वाले और आगामी जन्म में फल देने वाले कर्म समुदाय का मूल अविद्या बताया है। जिन कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है, उनको द्रष्टजन्मवेदनीय कहते हैं और जिन कर्मों का फल आगामी जन्मों मे मिलता है उनको अदृष्टजन्मवेदनी कहते हैं।
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्।
( वितर्काः ) वितर्क है ( हिंसा-आदयः ) हिंसा आदि [ यम नियमों के विरोधी भाव ] ( कृत-कारित-अनुमोदित ) स्वयं किये हये, दूसरों से करवाये हुये और समर्थन किये हुए ( लोभ-क्रोध-मोहपूर्वकाः ) लोभ-क्रोध-मोह कारण वाले ( मृदु-मध्य-अधिमात्रा ) मन्द, मध्य, और तीव्र भेद वाले ( दुःख-अज्ञान-अनन्तफलाः ) अत्यधिक दुःख और अत्यधिक अज्ञान फल वाले ( इति ) इस प्रकार ( प्रतिपक्ष- भावनम् ) प्रतिपक्ष का विचार करे अर्थात् दूर रहने का प्रयत्न करे।
उन में से हिंसा – की गयी, करवायी गई और अनुमोदित की गई इस प्रकार त्रिविध है । इन में से एक एक फिर तीन प्रकार की है। मांस चर्म के लिए की हुयी हिंसा लोभ से। इसने अपकार किया इस भावना से की हुई हिंसा क्रोध से। इस हिंसा से मुझे धर्म ( पुण्य ) मिलेगा ऐसी भावना से की हुयी हिंसा मोह से। लोभ, क्रोध, मोह भी मृदु ( मन्द ), मध्य ( पहले से अधिक ), अधिमात्र ( सबसे अधिक ) ऐसे तीन – तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार हिंसा के सत्ताईस भेद होते हैं।
वितर्कों में से हिंसा के विषय में इस प्रकार समझना चाहिए कि हिंसा तीन प्रकार है – कृत ( स्वयं की हुई ), कारित ( अन्य से करवाई हुई ) और अनुमोदित ( किसी के द्वारा की गई हिंसा को उचित मानना ) । लोभ, क्रोध और मोह, ये हिंसा के तीन कारण हैं। लोभ से कृत, लोभ से कारित, लोभ से अनुमोदित। इसीप्रकार क्रोध से कृत, कारित, अनुमोदित। मोह से कृत, कारित, अनुमोदित। ये ९ भेद हुए। कारणों के स्तर के भेद से हिंसा तीन प्रकार की होती है – अल्प लोभ से, मध्य स्तर के लोभ से, अधिक लोभ से की हूई हिंसा। अल्प क्रोध से, अध्यम स्तर के क्रोध से और अधिक क्रोध से की गई हिंसा। अल्प मोह से मध्यम स्तर के मोह से और अधिक मोह से की गई हिंसा। इस प्रकार के कारणों के भेद से कृत हिंसा के ९ भेद हो जायेंगे। इसी प्रकार कारित तथा अनुमोदित हिंसा के ९-९ होने पर २७ प्रकार की हिंसा हुई। पुनः इनके भी मृदु, मध्य, अधिमात्र भेद होने से हिंसा ८१ प्रकार की होती है। इसी प्रकार असत्य आदि के विषय में भी जानना चाहिए।
कर्मों को और अच्छे से समझने के लिए दार्शनिकों ने कर्मों को तीन भागों में बाँटा है – क्रियमाण कर्म, सञ्चित कर्म और प्रारब्ध कर्म।
क्रियमाण कर्म – जो वर्तमान में किया जाता है, सो क्रियमाण कर्म कहा जाता है। अर्थात् हम जो भी कर्म करते हैं मन, वाणी और शरीर से शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म यह सब क्रियमाण कहलाता है।
सञ्चित कर्म – जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है वे सञ्चित संस्कार ( कर्म ) कहाते हैं। अर्थात् सञ्चित वे संस्कार व वासना हैं जो किये जाते रहे कर्मों से उत्पन्न हुए हैं परन्तु जिनका फल अभीतक नहीं भोगा गया वे आत्मा में संस्कार व वासना रूप में एकत्रित ( सञ्चित ) रहते हैं।
प्रारब्ध कर्म – जो पूर्व किये हुए कर्मों के सुखदुःखस्वरूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अर्थात् अगणित सञ्चित संस्कारों में से जो संस्कार सद्यः फलोन्मुख होते हैं उनके अनुरूप किसी विशेष योनि में आत्मा देह धारण करता है। इस जन्म अथवा जीवन काल के प्रारम्भक होने के कारण इन संस्कारों का नाम प्रारब्ध है।
प्रारब्ध को ही पौराणिक भाषा में भाग्य कहते हैं । उपरोक्त प्रसंग को अच्छे से समझने के बाद यदि यह प्रश्न किया जाय कि कर्म बड़ा या भाग्य ? तो उत्तर कर्म बड़ा है यही आयेगा क्योंकि कर्म से ही भाग्य ( प्रारब्ध ) का निर्माण होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं।
पिछली चर्चा में कर्म के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया था । इस चर्चा में कर्म के फल का वर्णन किया जायेगा। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि कर्मों का फल कौन देता है, जीव को कर्मों का फल कैसे मिलता है।
कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, किसी भी अनुष्ठान से पाप कर्मों के फल में परिवर्तन नहीं होता –
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि।।
( ब्रह्मवैवर्तपुराण)
अच्छा या बुरा कर्मफल अवश्य ही भोगना पड़ता है चाहे जितना भी समय हो जाय बिना भोगे कार्य की समाप्ति नहीं होती है।
आत्मना विहितं दुःखमात्मना विहितं सुखम्।
गर्भशय्यामुपादाय भुज्यते पौर्वदेहिकम् ।। ( महाभारत )
दुःख अपने ही किये हुए कर्मों का फल है और सुख भी अपने ही पूर्व कृत कर्मों का परिणाम है। जीव माता की गर्भशैया में आते ही पूर्व शरीर द्वारा उपार्जित सुख-दुःख का उपभोग करने लगता है।
तत्काल फल न मिले तो भ्रमित न होवें। बीज बोने पर फल पाने में कुछ समय लग जाता है, इसी प्रकार कर्म का फल मिलने में थोड़ी देर लगने से अधीर लोग आस्था खो बैठते हैं। और ऐसा हो जाय कि शुभ कर्म करते हुए दुःख प्राप्त हो तो यह ना समझे कि परमेश्वर की कैसी व्यवस्था है , हमें दुःख क्यों मिल रहा है। इस पर एक भजन की पंक्तियाँ पढ़िये सब समझ में आजायेगा।
शुभ कर्म करते हुए दुःख भी अगर पारहे ।
पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे।।
आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिये।
हसते मुस्कुराते हुए ज़िन्दगी गुजारिये।।
इसीप्रकार जो बुरे कर्म करते हुए सुख पारहे हों तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि अभी पिछले शुभ कर्मों का फल मिल रहा है इस समय जो बुरे कर्म हम कर रहे हैं उनका भी फल एक दिन अवश्य मिलेगा। जो दुष्कर्म के दण्ड से बचे रहने की बात सोचने लगते हैं। कर्मफल मे विलम्ब होने के कारण जो यह विचार करते हैं कि कभी भी कर्मों का फल नहीं मिलेगा , उन्हें महर्षि व्यास की बात ध्यान देकर समझनी चाहिए। उन्होंने कहा –
नाधर्मः कारणापेक्षी कर्तारमभिमुञ्चति।
कर्ताखलु यथा कालं ततः समभिपद्यते॥ ( महाभारत)
अधर्म किसी भी कारण की अपेक्षा से कर्ता को नहीं छोड़ता निश्चय रूप से करने वाला समयानुसार किये कर्म के फल को प्राप्त होता है।
यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्॥
तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति।
( महाभारत )
जैसे बछड़ा हजार गौओं में अपनी माँ को पहचान लेता कर उसे पा लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता के पास पहुंच जाता है।
यदाचरति कल्याणि ! शुभं वा यदि वाऽशुभम्।
तदेव लभते भद्रे ! कर्ता कर्मजमात्मनः॥ ( रामायण )
सीता जी को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि हे मङ्गलमयी सीते ! मनुष्य जो अच्छा या बुरा कर्म करता है, अपने उसी किये कर्म के वैसे ही फल को प्राप्त किया करता है।
रामायण के अरण्यकाण्ड में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि पहले जन्म में हमने इच्छानुसार बारम्बार बहुत सारे पाप कर्म किये हैं, आज उनका फल मिल रहा है, इसी कारण हमारे ऊपर दुःख पड़ रहे हैं। राज्य का नाश होना, पिताजी का मरण, माता जी का वियोग होना, बन्धु बान्धवों से छूटना, यह सब बातें याद आती हैं तो हमारे शोक के वेग को परिपूर्ण कर देती हैं।
जन्म-जन्मन्यभ्यस्तं दानमध्ययनं तपः ।
तेनैवाऽभ्यासयोगेन तदेवाभ्यस्ते पुनः ।।
( चाणक्य नीति )
जन्म-जन्मान्तर से प्राणी ने दान देने तथा शास्त्रों के अध्ययन और तप करने का जो अभ्यास किया है, नया शरीर मिलने पर उसी अभ्यास के कारण ही वह सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। अतः मनुष्य को अपना भावी जन्म सुधारने के लिए इस जन्म में शुभ कर्मों के अनुष्ठान का अभ्यास करना चाहिए।
येन येन यथा यद्यत् पुरा कर्म समीहितम्।
तत्तदेकतरो भुङ्क्ते नित्यं विहितमात्मना।।
( महाभारत )
जिस जिस ने भी पहले जिस प्रकार से जो जो भी कर्म किया है, वह वह अपना किया कर्म करने वाला सदैव अकेला ही भोगता है, दूसरा उसका साथ नहीं देता।
एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः |
भोक्तारो विप्र मुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ||
( महाभारत )
पाप तो एक आदमी करता है, परन्तु उससे लाभ अनेक लोग उठाते हैं। लाभ उठाने वाले पापी नहीं कहलाते, पर केवल पाप करने वाला ही पापी कहलाता है।
कर्म चैव हि सर्वेषां करणानां प्रयोजनम्।
श्रेयः पापीयसां चात्रफलं भवति कर्मणाम्।।
( रामायण)
सभी इन्द्रियों का प्रयोजन कर्म ही है। अच्छे अथवा बुरे कर्मों का इस संसार में ही अच्छा या बुरा फल देखा जाता है।
दारिद्रयरोग दुःखानि बन्धन व्यसनानि च।
आत्मापराधवृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम्।।
( पञ्च तन्त्र)
गरीबी, बीमारियां, अन्य प्रकार के दुःख, कैद और संकट ये सब प्राणियों के निजी किये गये अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं।
भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं, सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य।
कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा, यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य।।
( नीति शतक )
जिस मनुष्य के पूर्वजन्म में किए शुभकर्मों का पुण्यफल प्रबल है, उसके लिए भयंकर वन भी श्रेष्ठ नगर बन जाता है, सब लोग उसके मित्र स्वजन बन जाते हैं और सारी पृथ्वी उसके लिए उत्तम निधियों और रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है।
कर्मणा जायते सर्वं कर्मैव गति साधनम्।
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत।। (विष्णु पुराण)
कर्म द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होता है और कर्म ही आगे बढ़ने का साधन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यथा शक्ति अच्छा कर्म ही करे।
कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी।
तथापि सुधियाऽऽचार्याः सुविचार्यैव कुर्वते ।।
( चाणक्य नीति )
मनुष्यों को कर्मानुसार ही फल प्राप्त होता है और बुद्धि भी कर्मानुसार ही बनती है तो भी बुद्धिमान लोग श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा सोचकर ही सभी कार्य करते हैं।
परमेश्वर ही कर्मों का फल देता है। चूंकि परमेश्वर न्यायकारी है इसीलिए सभी जीवों को सभी कर्मों का फल यथायोग्य अवश्य देता है। कर्म का फल कम या अधिक मिले, ऐसा नहीं होता है। कर्मों का फल न मिले, ऐसा नहीं होता है। किसी भी अनुष्ठान से किये कर्मों के फल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात् कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। किसी के कर्मों का फल किसी को मिले, ऐसा भी नहीं होता है। परमेश्वर की कर्मफल व्यवस्था को इस चर्चा में समझने का प्रयास करेंगे।
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः।
( क्लेश-मूलः ) अविद्यादि क्लेश हैं मूल = कारण जिस कर्म समुदाय के वह ( कर्माशयः ) कर्मसमुदाय ( दृष्ट-अदृष्ट-जन्म-वेदनीयः ) वर्तमान तथा भावी जन्म में भोग्य=फल देने वाला होता है ।
अर्थात् कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आगामी जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल शीघ्र और कुछ कर्मों का फल विलम्ब से मिलता है। जिन कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, उनको दृष्टजन्मवेदनीय कहते हैं और जिन कर्मों का फल आगामी जन्मों में मिलता है, उनको अदृष्टजन्मवेदनीय कहते हैं।
कर्म समुदाय को कर्माशय कहते हैं। शुभ कर्म समुदाय को पुण्य कर्माशय और अशुभ कर्म समुदाय को पाप कर्माशय कहा जाता है। पुण्य कर्माशय सुख देता है और पाप कर्माशय दुःख देता है। ऋषि पतञ्जलि कहते हैं –
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः।
( सति मूले ) अविद्यादि क्लेशों के विद्यमान रहने पर ( तद्-विपाकः ) उस कर्म समुदाय का फल ( जाति-आयुः-भोगाः ) जाति, आयु और भोग होते हैं। अर्थात् कर्माशय ( कर्म समुदाय ) के तीन फल हैं – जाति, आयु, भोग।
जाति = मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मकौड़े आदि का शरीर।
आयु = जन्म से लेकर मरणपर्यन्त काल आयु है।
भोग = भोग शब्द का अर्थ यद्यपि सुख दुःख भी है परन्तु इस प्रसंग में भोग शब्द का अर्थ ‘सुख दुःख प्राप्ति के साधन’ है जैसे धन सम्पत्ति, सोना-चांदी, भोजन-वस्त्र, पुत्र-परिवार आदि।
अदृष्ट जन्म में फल देने वाला कर्माशय ( अदृष्टजन्मवेदनीय ) जाति, आयु, और भोग तीन फलों का कारण होता है।
इस जन्म में फल देने वाला कर्माशय ( दृष्टजन्मवेदनीय ) आयु और भोग दोनों फलों को देने वाला होता है। दृष्टजन्मवेदनीय अर्थात् इस जन्म में फल देने वाला कर्माशय उपर्युक्त रूप से निश्चित फल वाला होता है तथा अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय निश्चित तथा अनिश्चित दोनों प्रकार के फल देने वाला होता है। जिस कर्म समुदाय का जाति आयु, भोग निश्चित हो जाता है, उसको नियतविपाक और जिसके जाति, आयु, भोग निश्चित नहीं हुये, वह अनियतविपाक है।
अनियतविपाक कर्माशय की तीन गतियाँ मानी जाती हैं।
पहली – कुछ कर्म बहुत लम्बे काल के पश्चात् फल देते हैं, कर्मों की इस गति को व्यासभाष्य में ‘नाश’ के नाम से कहा गया है।
दूसरी – किसी प्रधान कर्म के साथ मिलकर कर्म अपना फल दे देता है।
तीसरी – जब प्रबल कर्म अपना फल देते हैं तो वह कर्म उनके नीचे दवा रहता है और अनुकूल वातावरण आने पर अपना फल देता है।
वास्तव में कोई भी कर्म बिना फल दिये नष्ट नहीं होता। कर्म और कर्मफल का जानना अति परिश्रमसाध्य है। किस कर्म का क्या, कितना कब, कैसे फल मिलेगा, इसको पूर्णरूपेण ईश्वर ही जान सकता है। आंशिक रूप से मनुष्य भी जान सकता है। आंशिक रूप में जानने से कर्म और कर्मफल पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। इससे मनुष्य शुभ कर्मों को श्रद्धापूर्वक करता है और अशुभ कर्मों को छोड़ देता है। शुभ कर्मों के किये बिना अशुभ कर्मों को छोड़ना कठिन है।
ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्।।
( ते ) वे जाति, आयु और भोग ( ह्लाद-परिताप-फलाः ) सुख और दुःख रूप फल वाले होते हैं ( पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात् ) पुण्य और पाप के कारण उत्पन्न होने से।
वे जाति, आयु और भोग पुण्य और पाप कारणजन्य होने से सुख और दुःख रुप फल वाले होते हैं अर्थात् जिन जाति, आयु, भोग का कारण पुण्य होता है, वे सुख देने वाले होते हैं तथा जिन जाति, आयु, भोगों का कारण पाप होता है, वे दुःख देने वाले होते हैं।
पुण्य कर्म करने वाले जीवों को विद्वान, धार्मिक सम्पन्न माता-पिता के घर में मनुष्य का जन्म मिलता है। वहां पर जाति, आयु, भोग सुखप्रद होते हैं। अपुण्य कर्म करने वाले जीवों को पशु आदि जन्म मिलता है। वहां जाति, आयु, भोग दुःखप्रद होते हैं।
पिछली चर्चाओं में हमने समझा कि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। परमेश्वर हमें कर्मों के फल के रूप में जाति, आयु और भोग प्रदान करता है। आज हम आयु,जाति और भोग पर कुछ विस्तार चर्चा करेंगे।
समाज में आयु के बारे में कुछ ऐसा प्रचार हुआ है कि आयु जन्म के साथ की निर्धारित हो जाती है, आयु न तो घटती है और न ही बढ़ती है, जिसकी मृत्यु जब होनी होती है तब ही होती है।
यदि हम उपरोक्त कथन को सही माने तो अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे – जब मृत्यु निर्धारित समय पर होनी ही है तो आयुष्मान भव, जीवेम शरदःशतम् आदि का क्या औचित्य रह जायेगा। यदि कोई किसी को मार दे तो मारने वाला दोषी क्यों कर होगा ? क्योंकि मरने वाले की तो मृत्यु होनी ही थी। ऐसे ही अनेक प्रश्न उपस्थित होंगे।
वैदिक सिद्धान्त के आधार पर मृत्यु तो निश्चित होती ही है लेकिन कब होती है या कब होगी यह निर्धारित नहीं होता। आयु को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है।
इस पर कुछ तर्क पूर्ण चर्चा करते हैं जैसा कि योग दर्शन में कहा है कि आयु कर्म के आधार पर प्राप्त होती है तथा दूसरी बात यह है कि कुछ कर्मों का फल वर्तमान जन्म में प्राप्त होता है और कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भी प्राप्त होता है।( यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी कर्मों के फल का निर्णय मृत्यु के बाद ही नहीं होता बल्कि कुछ कर्मों का फल जीवन चलते भी प्राप्त हो जाता है।) अब इन दोनों बातों को साथ साथ जोड़कर देखते हैं अर्थात् जन्म के समय जो आयु प्राप्त होती है वह पिछले जन्मों के कर्मों का फल है साथ ही इस आयु को वर्तमान के कर्म भी प्रभावित करेंगे। वर्तमान जीवन में किये जाने वाले कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आयु को घटा और बढ़ा सकते है क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इसी जन्म में करने पर इसी जन्म में आयु देने वाले होते हैं।
इसीलिए वेदों में सौ वर्ष और उससे भी अधिक जीने की बात कही है। आयुर्वेद ऐसा उपवेद है जो आयु पर ही लिखा गया है। आयुर्वेद में अनेक ऋषियों ने आयु को बढ़ाने के लिए शुभ कर्म, अच्छा भोजन, सही नींद, ब्रह्मचर्य का पालन और व्यायाम आदि वर्णन किया है। अर्थात् शुभ कर्म “= पुण्य कर्म = वेदोक्त कर्म करके, आयुर्वेद के आधार पर शरीर को स्वस्थ रखने वाला – वात-पित्त-कफ को सम रखने वाला भोजन करके, रात्रि में उचित समय से गहरी नींद लेकर, ब्रह्मचर्य के पालन और नित्य व्यायाम – आसन – प्राणायाम आदि करके आयु को बढ़ाया जा सकता है और इसके विपरीत चलकर आयु घट जाती है।
इसीप्रकार भोग के सन्दर्भ में समझना चाहिए अर्थात् जन्म के समय सुख-दुःख के जो साधन मिलते हैं वे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है उन साधनों भी घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है।
यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है – चोरी, डकैती, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि अनैतिक पापाचरण से प्राप्त धन सुख का साधन नहीं हैं ।
यदि कोई ऐसा प्रश्न करे – समाज में व देश में चोरी करने वाले, रिश्वत लेने वाले, मिलावट करने वाले, अधिक मुनाफा लेने वाले, झूठी गवाही, असत्य, छल-कपट आदि गलत कार्यों को करके धन, सम्पत्ति इकट्ठी करने व गलत कार्य करने वाले व्यक्ति सुखी दिखाई देते हैं। क्या ईश्वर उनको देखता नहीं है? दण्ड नहीं देता? जब ऐसे गलत कार्य करने वाले सुखी देखे जाते है तो धर्म, सदाचार, नैतिकता पर से लोगों का विश्वास ही हट जाता है और अन्य लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करके उनकी तरह बुरे काम करने लग जाते है और इससे सारे समाज, राष्ट्र में भ्रष्टाचार फैल जाता है जो आज हम स्पष्ट देखते है।
उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है – मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है वह अच्छा, बुरा जैसा चाहे अपनी इच्छा से कर सकता है। झूठ, छल-कपट, चोरी, मिलावट, रिश्वत, शोषण, अन्याय आदि के द्वारा वह क्या प्राप्त करेगा? रूपया-पैसा। इन रुपयों से वह अच्छा मकान, गाड़ी, वस्तु, भोजन, मनोरंजन के साधनों को प्राप्त करके भी क्षणिक सुख ही तो पाता है। किन्तु इन साधनों व साधनों के पीछे बुरे कर्मों से प्राप्त धन का जो दोष है, पाप है उसका डंक, विष व उसकी आग उसे अन्दर ही अन्दर चुभती, जलाती रहती है।
महाराज मनु कहते हैं –
अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ।।
मनुष्य ( अधर्मेण तावत् एधते ) अधर्माचरण के द्वारा पहले पहले उन्नति करता है, ( ततः भद्राणि पश्यति ) उससे वह अपना कल्याण=सुख-सुविधा-मान-प्रतिष्ठा प्राप्ति होते हुए भी अनुभव करता है, (ततः सपत्नान् जयति ) उससे शत्रुओं पर भी बढ़ोतरी प्राप्त करता है ( तु ) किन्तु अन्ततः उस अधर्मकर्ता का ( समूलः विनश्यति ) जड़ से ही सर्वनाम हो जाता है।
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रसंग पर लिखते हैं – जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसे तालाब के बाँध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पांखड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खंडन, और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है और धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात् शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही अधर्मी नष्ट हो जाता है।
मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसा गाय आदि की सेवा का फल दूध शीघ्र प्राप्त नहीं होता वैसे ही किए हुए अधर्म का फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता किन्तु वह किया हुआ अधर्म धीरे-धीरे कर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है पश्चात् अधर्मी दुख ही दुख भोगता है। इसलिए यह कभी नहीं समझना चाहिए कि कर्त्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होता है।
[ आज की चर्चा को पढ़कर आपको यह लगेगा कि वैदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध व्यवहार करने से समाज कितनी भयंकर स्थिति में आगया है और अभी भी नहीं सभला या नहीं सभाला गया तो कितने भयंकर परिणाम आयेंगे।
समाज की इस विनाशकारी स्थिति को देखकर हम सभी को यह भी विचार करना पड़ेगा कि वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए ( जिससे समाज का कल्याण हो सके ) आर्य समाज की कितनी बड़ी आवश्यकता है। ]
कर्मों का फल जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। पिछली चर्चा में आयु और भोग पर थोड़ा विचार विमर्श लिखा, ( भोग पर विस्तार से आगे लिखेंगे ) आज जाति पर लिखते हैं।
प्रथम तो यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान में जिसके के लिए जाति शब्द प्रयोग किया जा रहा है वह जाति नही हैं बल्कि वैदिक वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप है। अर्थात् जाट, गुर्जर, यादव, पण्डित आदि जाति नहीं है यह तो प्राचीन वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य आदि का बिगड़ा हुआ रूप है या वंश परम्परायें हैं। प्राचीन काल में वैदिक मर्यादाओं के कारण योग्यता और कर्म के आधार पर वर्ण प्रदान किये जाते थे जो आज कल जन्म के आधार पर माने जाने लगे हैं, जो कि ठीक नहीं है इससे ऊंच नीच का भेदभाव जैसे अनेक दोष समाज में उपस्थित होकर मानवता की बहुत हानि होती है/होरही है।
महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज जाति के सन्दर्भ में आर्योद्देश्यरत्नमाला में लिखते है – “जो जन्म से लेकर मरण पर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात् मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि समूह हैं, वे ‘जाति’ शब्दार्थ से लिये जाते हैं।
न्याय सूत्र यही कहता है –
“समानप्रसवात्मिका जाति:”
अर्थात् जिनके जन्म का मूल स्त्रोत सामान हो (उत्पत्ति का प्रकार एक जैसा हो) वह एक जाति बनाते हैं ।
हर जाति विशेष के प्राणियों में शारीरिक अंगों की समानता पाई जाती है। एक जन्म-जाति दूसरी जाति में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती है और न ही भिन्न जातियां आपस में सन्तान उत्त्पन्न कर सकती हैं। अतः जाति ईश्वर निर्मित है। जैसे विविध प्राणी हाथी, सिंह, खरगोश इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं। इसी प्रकार संपूर्ण मानव समाज एक जाति है।
शब्दव्युत्पत्ति की दृष्टि से जाति शब्द संस्कृत की ‘जनि’ (जन) धातु में ‘क्तिन्’ प्रत्यय लगकर बना है।
अर्थात् जाति का अर्थ है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण |
इन परिभाषाओं और शब्दव्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि ‘जाति’ शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में विभिन्न मानवजातियों के लिये नहीं होता था।
कृपया ध्यान दें –
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः।
( सति मूले ) अविद्यादि क्लेशों के विद्यमान रहने पर ( तद्-विपाकः ) उस कर्म समुदाय का फल ( जाति-आयुः-भोगाः ) जाति, आयु और भोग होते हैं। अर्थात् कर्माशय ( कर्म समुदाय ) के तीन फल हैं – जाति, आयु, भोग।
जाति = मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, मकौड़े आदि का शरीर।
यहां बहुत अच्छे से यह समझना है कि योग दर्शन में जाति का अर्थ शरीर से है मनुष्य, पशु आदि। और यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि यह जाति ( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का शरीर ) भी आत्मा को कर्मों के आधार प्राप्त होता है। यह विषय बहुत विस्तार चाहता है इसीलिए विषय को स्पष्ट करने के लिए यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में संसार में क्या क्या मान्यतायें प्रचलित हैं और उनसे क्या क्या हानि हो सकती हैं।
आप संसार के विभिन्न लोगों से पूछिये कि मरने के बाद क्या होगा ( शरीर के सन्दर्भ में ) ? अर्थात् किसका शरीर मिलेगा? या आत्मा किस योनि में जायेगा ? तो आपको विभिन्न उत्तर मिलेंगे। आज आप उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए तब आपको पता चलेगा कि वैदिक सिद्धान्तों की कितनी आवश्यकता है।
० एक मानसिकता = संसार में कुछ लोग ऐसे है जो यह कहते हैं कि आत्मा को प्रत्येक बार एक जैसा ही शरीर मिलता है अर्थात् यदि आत्मा ने मनुष्य का शरीर छोड़ा है तो अगले बार भी उसे मनुष्य का शरीर ही मिलेगा। और मनुष्य में भी पुरुष का शरीर छोड़ा है तो पुरुष का और यदि स्त्री का शरीर छोड़ा है तो स्त्री का शरीर ही प्राप्त होगा। कुत्ते का शरीर छोड़ा है कुत्ते का शरीर ही मिलेगा। पक्षी का शरीर छोड़ा है तो पक्षी का ही शरीर मिलेगा।
आप चिंतन करेंगे यहां पर अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। जैसे –
– कोई आत्मा मनुष्य शरीर को पाकर जीवन भर पाप कर्म ही करता रहे तो भी क्या उसे अगले बार मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा ?
अगला प्रश्न और भी मनोवैज्ञानिक है यदि कोई मनुष्य ऐसा विचार कर ले, ऐसा पूर्ण विश्वास कर ले, कि मैं अगले बार निश्चित रूप से मनुष्य ही बनुंगा तो वह शेष जीवन में कैसे ( पाप या पुण्य ) काम करेगा ?
इस प्रश्न का मनोवैज्ञानिक उत्तर ढूंढा जाय तो उत्तर मिलेगा कि जो मनुष्य अपने मस्तिष्क में ऐसा निश्चय कर लेगा कि मैं हर बार मनुष्य ही मनुंगा तो वह शेष जीवन में पापाचरण ही करेगा। क्योंकि पुण्य कर्म का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा।
० दूसरी मानसिकता = संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं आत्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो चौरासी लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है अर्थात् अभी अगले बार मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद फिर जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त होगा। आइए इस मानसिकता का भी विश्लेषण करते हैं। यहां भी कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। जैसे –
जो आत्मा मनुष्य शरीर को पाकर जीवन भर पुण्य कर्म ही करता रहे तो भी क्या उसे अगले बार मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा ?
अगला प्रश्न मनोवैज्ञानिक है। यदि कोई मनुष्य ऐसा निश्चय कर ले कि कैसे भी मैं अगले बार मनुष्य नहीं बनूंगा तो वह शेष जीवन में पाप करेगा या पुण्य करेगा ?
इस प्रश्न के उत्तर में विश्लेषणात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जो मनुष्य ऐसा मान बैठता है कि मैं अगले बार मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं करूंगा या मनुष्य नहीं बनूंगा तो वह निश्चित रूप से शेष जीवन में पाप ही करेगा। क्योंकि यहां भी पुण्य कर्मों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
ऐसी ही अनेक मान्यतायें संसार में प्रचलित है। यहां एक मान्यता का और उल्लेख करते हैं।
० अगली मानसिकता = ऐसे भी लोग संसार में हैं जो यह मानते हैं कि अगला तो जन्म होता ही नहीं है। यदि उनसे यह पूछा जाए कि अगला जन्म नहीं होता है तो क्या होता है ? कुछ तो होता होगा ? इस पर उनका कहना है कि या तो जन्नत ( स्वर्ग ) मिलता है या दोजख ( नरक ) मिलता है। यदि उनसे फिर प्रश्न किया जाए की जन्नत या दोजख कैसे मिलता है? किस आधार पर मिलता है? तो उनका कहना है कि जो हमारी बात मानते हैं उनको जन्नत मिलता है, जो हमारी बात नहीं मानते हैं उनको दोजख मिलता है।
अब आप स्वयं ही निर्णय कीजिए कि इन बातों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने पर कितने विनाशकारी परिणाम आते हैं। लोग जन्नत पाने के लिए पशुओं और अन्य जीवों के साथ साथ मनुष्यों को भी मार देते हैं।
उपरोक्त विचारधाराओं के समझने के बाद आपके मन में प्रश्न होगा कि सही विचारधारा क्या है? सैद्धान्तिक रूप से क्या सही है? इस पर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में वेद का प्रमाण देते हुए उल्लेख किया है –
द्वे सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्।
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च। ( यजुर्वेद १९/४७ )
इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को सुनते हैं। एक मनुष्य शरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष आदि का होना।
इसमें मनुष्य शरीर के तीन भेद हैं – एक पितृ अर्थात् ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात् सब विद्याओं को पढ़कर विद्वान होना, तीसरा मर्त्य अर्थात् साधारण मनुष्य का शरीर धारण करना।
इनमें प्रथम गति अर्थात् मनुष्यशरीर पुण्यात्माओं और पुण्यपाप तुल्य वालों को होता है, और दूसरा जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिये है। इन्हीं भेदों से सब जगत के जीव अपने अपने पुण्य और पापों के फल भोग रहे हैं। जीवों को माता और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्मधारण करना, पुनः शरीर को छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, बारम्बार होता है।
यहां पूर्णतया स्पष्ट है कि –
पुण्य अधिक = मनुष्य शरीर
पुण्य पाप समान = मनुष्य शरीर
पाप अधिक = मनुष्येतर शरीर अर्थात् मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य शरीर ( पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादि )
इस मान्यता पर आप कितने भी प्रश्न करेंगे तो उत्तर ठीक ही आयेगा।
शरीर कर्मों के आधार पर प्राप्त होगा। हर बार यदि पुण्य कर्म अधिक होंगे तो हर बार मनुष्य का शरीर मिल जायेगा। यदि पाप अधिक होंगे तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी पुण्य कर्म करने के लिए ही प्रयास करेंगे। पाप कर्मों से बचेंगे। इसी से संसार का कल्याण होगा। इसीलिए इसी सिद्धान्त के प्रचार की महती आवश्यकता है।


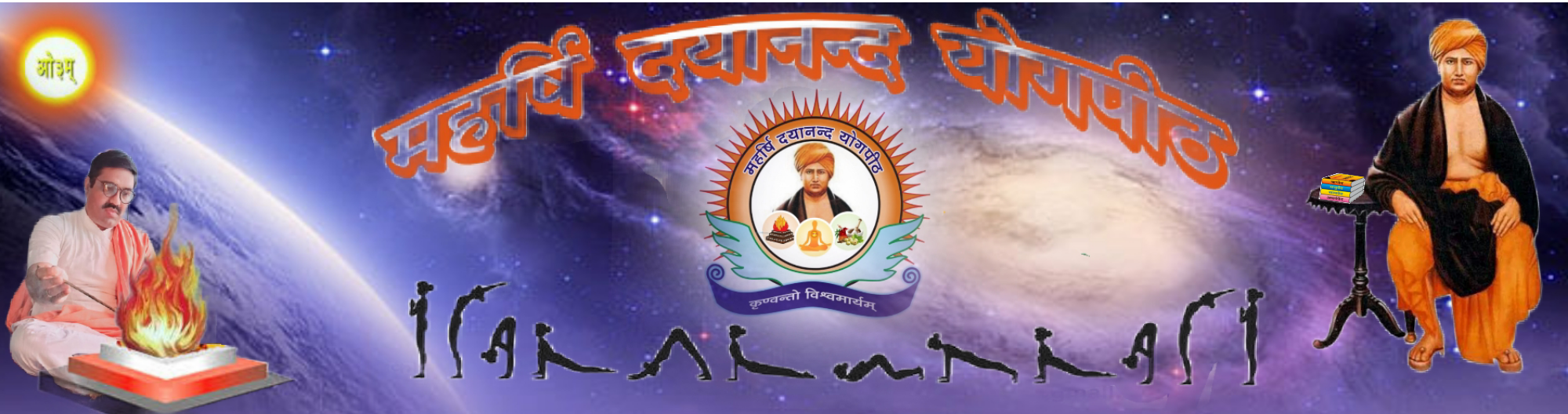


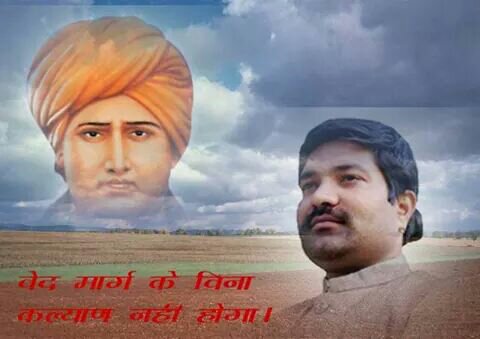

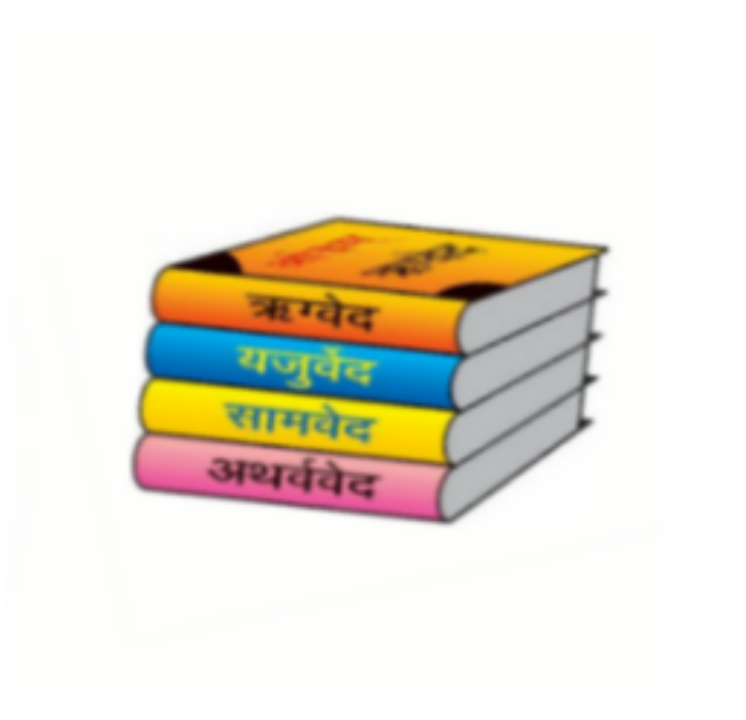
अति उत्तम प्रयास, वैदिक सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए आधुनिक संयंत्र को माध्यम बनाकर युवाओं तक पहुंचाने एक उत्तम साधन।
प्रशिक्षण के लिए ६ जनवरी २०२५ से सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को रात्रि ८:०० बजे ९:०० बजे तक गूगल मीट पर ओन लाइन कक्षा रहेगी।
कक्षा के लिए लिंक निम्नलिखित है जिसे क्लिक करके आप जुड़ सकेंगे –
https://meet.google.com/pjs-kszi-gdm
इच्छुक भाई/बहन व्यवहार भानु, संस्कार विधि , एक नोटबुक या डायरी ( दैनन्दिनी ) और पेन ( लेखनी ) के साथ कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।